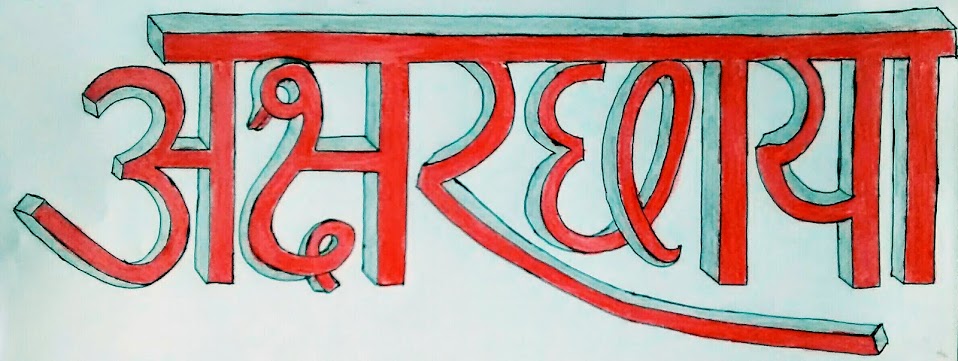किसी पत्रिका को खरीदते समय हमारी नजर उसके नाम के साथ जुड़ी टैग लाईन पर भी जाती है। देखकर पता चलता है कि पत्रिका तो जनसंघर्ष से सरोकार रखती है, पर अंदर की सामग्री देख हम ठगे रह जाते हैं। अभिजन की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती ऐसी पत्रिकाएं पूर्णतः प्रायोजित होती हैं जिनके संपादक महानगरों के वातानुकूलित कमरे में बैठ सत्ता एवं कुलीन वर्ग के साथ कदम–दर–कदम चलकर चैन की वंशी बजाते हैं। सत्ता आखिर इससे अधिक क्या चाहेगी ?
अगर सत्ता एवं उसकी मशीनरी इन कुपंथियों के कारण आश्वस्त रहे तो फिर जनचेतना का नेतृत्व कौन करेगा ? प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य राजनीति के आगे–आगे चलने वाली मशाल है, पर आज के परिदृश्य को देखकर लगता है कि साहित्य राजनीति की धुरी पर लगातार चक्कर लगाती जा रही है जिसके केंद्र में सत्ता है। ऐसी स्थिति में साहित्य को बचाने का दारोमदार लघु पत्रिकाओं पर आ जाता है। वे ही जन–सरोकार की बातों को सामने लाती हैं।
लघु पत्रिका आन्दोलन की शुरुआत आजादी के पश्चात उस समय शुरू हुई जब रचनाकारों के एक वर्ग ने महसूस किया कि सत्ताश्रयी एवं सेठाश्रयी पत्रिकाएं वैचारिक दवाब एवं अपने व्यवसायिक हितों के चलते एक ही तरह की रचनाएं छाप रही हैं तथा उनकी स्थिति रुढ हो गई है। नव विचारों की ग्रहणीयता उन्हें मंजूर नहीं थी तथा साहित्यिक विधा में नया प्रयोग करना खतरे से खाली न था। ऐसे समय में परिवर्तनकारियों के छोटे–छोटे समूहों ने अपने सहयोग एवं प्रतिबद्धता की बदौलत 'लघु पत्रिका' आन्दोलन की शुरुआत कर दी। चाहे अकविता/अकहानी का दौर हो या साठोतरी कहानी की धमक, नई कविता/नई कहानी का आन्दोलन या वामपंथ विचारधाराओं का दौर...बड़ी पत्रिकाएं इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाती थीं। इस कारण प्रतिबद्ध रचनाकारों के छोटे–छोटे समूहों ने आपसी सहयोग, सीमित बजट एवं छोटे स्तर पर प्रचार–प्रसार की बदौलत अपनी वैचारिकता एवं प्रतिरोध को लघु पत्रिकाओं में दर्ज करना शुरू कर दिया तथा यह काफी सफल भी हुआ। ये पत्रिकाएं मुख्यतः सत्ता एवं पूँजीवाद का प्रतिरोध करती हैं तथा जन–सरोकार एवं जन–चेतना को विस्तार देती हैं। जीवन के अधूरेपन को विभिन्न विधाओं में व्यक्त करने का कार्य साहित्यिक एवं वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध रचनाकारों द्वारा किया जा रहा है। लघु पत्रिकाओं का सीमित बजट इसके विस्तार एवं प्रसार में बाधा बनती है, पर वैचारिक प्रतिबद्धता इसे बनाए रखती है। लोक के प्रति समर्पित बांदा से निकलने वाली पत्रिका 'लोकविमर्श 2' के प्रथम पृष्ठ पर छपा नोट लघु पत्रिका आन्दोलन के ईमानदार प्रयास को स्वतः व्यक्त कर देती है―" पत्रिका निजी संसाधनों से संचालित है। किसी भी तरह का विज्ञापन व आर्थिक सहयोग किसी संस्था से नहीं लिया जाता...साथ ही संपादकीय टीम के सभी सदस्य अवैतनिक हैं। पत्रिका से किसी भी किस्म का कोई आर्थिक लाभ किसी सदस्य को प्राप्त नहीं होता है।" वहीं यह भी सत्य है कि कुछ पत्रिकाएं आज सत्ता एवं व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा प्रायोजित हैं तथा खूब फल–फूल रही हैं। पर यह समय निराश होने का नहीं है। आज हमारे बीच कई लघु पत्रिकाएं पूरे उत्साह से लोक के प्रतिरोध को रच रही हैं...साहित्य को अभिजात्य विचारधारा की जकड़न से मुक्त कर रही हैं। जनपथ, कृतिओर, लहक, यात्रा, अनहद, लोकविमर्श, दुनिया इन दिनों, बाखली एवं लोकोदय जैसी लघु पत्रिकाएं इस समय हिंदी साहित्य में अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक कर रही हैं।
बिहार के आरा से निकलने वाली पत्रिका 'जनपथ' आज परिचय की मोहताज नहीं है। अनंत कुमार सिंह के संपादन में यह आज बड़ी दृढता से जन के पक्ष में खड़ी है। सच तो यह है कि 'जनपथ' अनंत दा की साधना है। आज के समय में जब आमजन की उम्मीदों को ध्वस्त करने की सर्वत्र तैयारी है...इस पत्रिका ने अपने दायित्व के निर्वहन कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। इस श्रंखला में अगली महत्वपूर्ण पत्रिका बदायूँ से छपने वाली 'कृतिओर' है जो लोकचेतना की सशक्त पक्षधरता का निर्वहन दृढतापूर्वक कर रही है। विजेन्द्र के संरक्षण एवं डॉ. अमीरचन्द वैश्य के संपादन में यह लोक–सरोकार के रचनाकारों को निरंतर जगह देती हुई आज के समय की एक जरूरी पत्रिका बनी हुई है।
गणेश पांडेय के संपादन में गोरखपुर से निकलने वाली पत्रिका 'यात्रा' सच में लोक की यात्रा कराती है। यह पत्रिका हाशिये पर रख दिए गए जन एवं उनके हिमायती रचनाकारों को अपना मंच प्रदान करती है। महानगरों के बड़े मठों के द्वारा साजिशन उपेक्षित लोक के महत्वपूर्ण रचनाकारों की रचनाएं इसमें शामिल होती हैं। यात्रा–11 इसी क्रम में छपकर निकली है जिसमें देश के विभिन्न भागों में जनसंघर्ष को अपनी आवाज देने वाले कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। जन-सरोकार वाली पत्रिकाओं की अगली कड़ी में नई दिल्ली से निकलने वाली पाक्षिक पत्रिका 'दुनिया इन दिनों' एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह मुख्यतः राजनीतिक एवं साहित्यिक–सांस्कृतिक खबरों एवं रचनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित करती है। लीक से हटकर अपनी विषय–विविधता, भाषाई आस्वाद एवं जमीन से जुड़े सरोकार के कारण इस पत्रिका का इंतजार पाठकों को बेसब्री से रहता है। साहित्य की हर विधा को अपने में समेटे सुधीर सक्सेना जैसे कवि के संपादन में यह लोक की सशक्त अभिव्यक्ति बन चुकी है।
इलाहाबाद से निकलने वाली 'अनहद' निश्चित रूप से साहित्य की साधना का परिणाम है। संतोष चतुर्वेदी के संपादन में इस पत्रिका ने आज अपनी साख साहित्यिक परिवेश में बना ली है। साहित्य की सभी विधाओं को सम्मिलित करते हुए उसकी गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य संपादक बखूबी कर रहे हैं। कोलकाता से निकलने वाली 'लहक' अपने उद्देश्य एवं कलेवर के प्रति सजग रहकर आगे बढने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका है। निर्भय देवयांश के संपादन में यह लोक की वैचारिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। एक तरफ लोक–संघर्ष की बात करनेवाली रचनाएं इसमें जगह पा रही हैं तो दूसरी तरफ लोक का मुखौटा लगाकर सत्ता की मलाई खाने वाले साहित्यकारों का सच इसके द्वारा सामने लाया जा रहा है।
लघु पत्रिकाओं के स्वरूप एवं सरोकार की चर्चा करते हुए इस साल लोक–चेतना एवं संघर्ष को मुख्य मुद्दा बनाकर उतरने वाली पत्रिकाओं में डॉ. गिरीश पांडेय 'प्रतीक' के संपादन में 'बाखली' का प्रवेशांक हमारे सामने आ चुका है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलने वाली पत्रिका के अंक ने साहित्यिक समाज को आकर्षित किया है। लोक–संस्कृति एवं उसके संघर्ष को व्यक्त करती यह पत्रिका लंबी राह की सहयात्री है। लोकोदय प्रकाशन, लखनऊ से छपकर जनपक्षधर लोकधर्मी साहित्य की त्रैमासिकी 'लोकोदय' आपके समक्ष पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। लोकविमर्श आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग बनी यह पत्रिका भावना मिश्रा के संपादन में साहित्य की विभिन्न विधाओं को समेटती हुई लोक के यथार्थ को सामने रख रही है।
अभी आप 'लोकविमर्श' स्वयं पढ रहे हैं; अतः इस संबंध में कुछ कहना मेरी वाचालता मानी जाएगी। जनवादी लेखक संघ बांदा के संपादन में यह आन्दोलन के रूप में अग्रसर है। संपादक द्वारा 'लोकविमर्श 1' में यह घोषणा की गई है―" यह सिर्फ पत्रिका नहीं बल्कि आन्दोलन है। यह आन्दोलन महानगरों से दूर रहनेवाले तथा आलोचकों की नजरों से ओझल प्रतिबद्ध रचनाकारों का है।" निश्चित ही इस पत्रिका ने उम्मीद बढा दी है। इसकी समीक्षा आप मुझसे बेहतर कर सकेंगे।
मेरी जानकारी की अपनी एक सीमा है। कोई जरूरी नहीं कि जनसरोकार वाली लघु पत्रिकाएं इतनी ही हैं या लोक का पक्ष सिर्फ यही सब ले रही हैं। कई सारी पत्रिकाएं आपकी नजरों से गुजरी होगी जिन्हें आप अपनी कसौटियों पर खरा मानते हों। बस वैचारिक रूप से सशक्त एवं जन–प्रतिरोध को अभिव्यक्त करनेवाली इन पत्रिकाओं को हमारा लगातार समर्थन मिलते रहना चाहिए ताकि लोक का पक्ष सत्ता एवं पूँजीवादी ताकतों की साजिश की धुंध में न खो जाए।