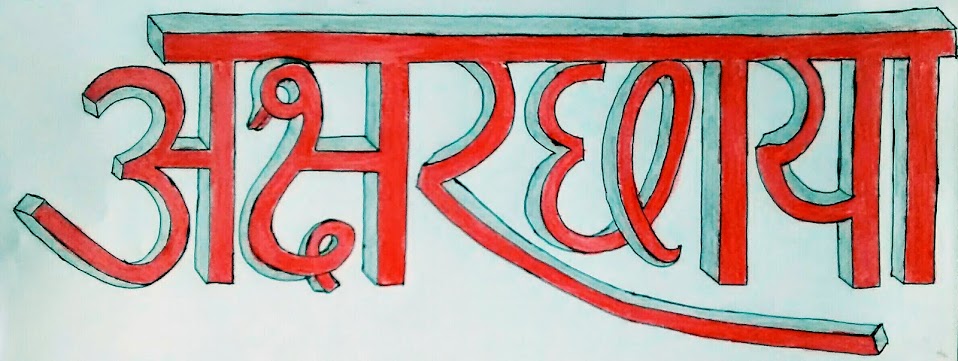यह अद्भुत संयोग था कि बिहार के सहरसा जिले के गांव महिषी में एक विद्रोही रचनाकार के जीवनरूपी दीपक की बाती से तेल शेष हो चला था, ठीक उन्हीं दिनों उसी गांव में एक नन्हा शिशु अपनी ज्योति से सभी दिशाओं को आलोकित कर रहा था। कौन जानता था कि आगे चलकर वह शिशु उस विद्रोही रचनाकार के जीवन एवं रचनाकर्म पर पड़ी धूल को झारने–पोंछनेवाला था जोकि समय एवं समाज की उपेक्षा से पड़ती चली गयी थी। महिषी के उस विद्रोही रचनाकार राजकमल चौधरी की कई दुर्लभ रचनाओं को आज के समय में हम पढ़ पा रहे हैं तो उसके पीछे वहां के उस शिशु के संघर्ष एवं अथक परिश्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी किसी भी रचना पर धैर्यपूर्वक काम करनेवाले मैथिली एवं हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार तारानन्द वियोगी की 'राजकमल चौधरी' के जीवन पर आधारित रचना 'जीवन क्या जिया!' तद्भव–33 के अंक में आ चुकी है। जब आप उस शिशु को पहचान ही गए हैं तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसने राजकमल चौधरी को जानने–समझने की कोशिश कैसे शुरू की। उस राह में क्या–क्या बाधाएं आईं तथा कौन लोग इस राह के संबल बने। 'जीवन क्या जिया' संस्मरण, जीवनी एवं उपन्यास के तत्वों को अपने में समेटे हुए है। इस रचना में एक तरफ राजकमल चौधरी तो दूसरी तरफ खुद तारानन्द वियोगी की कहानी एक-दूसरे के समानांतर चलती है जिन्हें जोड़ती है...वियोगी जी का समर्पण एवं वह उद्देश्य कि महिषी को सिर्फ मंडन मिश्र की वजह से ही नहीं बल्कि राजकमल चौधरी की वजह से भी जाना जाए। इस रचना के अंश आविर्भाव, उत्कर्ष एवं प्रस्थान शीर्षक से एक–एक कर आपके समक्ष आते जाएंगे। आज आविर्भाव !
–बाबा वो फूल बाबू थे न, मधुसूदन बाबू के लड़के–वो बहुत बड़े लेखक थे । ‘राजकमल चौधरी’ कहलाते थे । देश भर में उनका बहुत नाम है । लेकिन, अपने गांव में उन्हें कोई नहीं जानता । लोग जानते भी हैं तो अच्छी तरह से नहीं । उनका जन्मदिन 13 दिसंबर को है । इस अवसर पर हमलोग उनकी जयंती मनाना चाहते हैं, बाबा । –सोलह सतरह आयु वर्ग के कुछ लड़के गांव के सर्वाधिक प्रतिष्ठित मान्यजन से कह रहे थे ।
–तो, उस जयंती में क्या सब होगा ?
–उसमें हम बाबा, मिथिला के कुछ बड़े बड़े विद्वानों को बुलाएंगे । कवियों को भी बुलाएंगे । राजकमल जी के बारे में लोग बताएंगे । फिर काव्यपाठ होगा ।
बाबा ने एक लंबी हुंकारी भरी, फिर चुप हो गए । हमलोग उनकी ओर देखते रहे ।
–तुम किसके बेटे हो ?
मैंने अपने पिता का नाम बताया । मेरे पिता का नाम सुनकर उनके चेहरे का भाव और अधिक तिक्त हो गया ।
–तुमलोग किसके किसके बेटे हो ?
सबने अपने अपने पिता का नाम बताया ।
बाबा बोले–सब लड़के तो गरीब घर के हो । चंदा लेना पड़ेगा ।
–जी बाबा, हमलोग चंदा के लिए ही आए थे ।
–चंदा तो खैर, हम नहीं देंगे । इस तरह के काम में हम किसी को चंदा नहीं देते हैं । तब, एक मदद कर देंगे ।
–क्या बाबा ?
–हम दरोगा जी को बोल देंगे कि तुमलोगों की पकड़ धकड़ नहीं करें ।
–सो क्यों बाबा ?
–देखो, बात ये है–––
शुद्ध मैथिलों की जो शैली है, उस शैली में, मिचरा मिचराकर बाबा कहने लगे–जयंती मनाने का कुछ नियम कायदा होता है । इसमें विचार किया जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को किस बात से शांति मिलेगी, क्या करोगे तो प्रसन्नता होगी । तो, तुमलोग थोड़ा अच्छा से करो ।
–जी बाबा, बताइए ।
–मिट्टी तेल वाले डीलर के पास जो ड्राम होता है, वो दो ठो ड्राम कहीं से मंगनी कर लो । उसमें भरवाकर देसी दारू मंगवा लो । पाव भर गांजा का भी कहीं से प्रबंध करना पड़ेगा । और ये सब लेकर, महिषी गांव का जो सिमान है न, वहां पर बैठ जाओ । हरेक आने जानेवाले मुसाफिर को एक एक डबूक दारू दो । गांजा पिलाओ । इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी । तुमलोगों का भी नाम होगा । श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हो बाबू, तो सच्ची श्रद्धांजलि दो । हम सारे लड़के अकबका गए कि बाबा यह क्या कह रहे हैं! किसी के भी मुंह से बकार तक नहीं निकल रहा था । टक टक हम बाबा का मुंह ताके जा रहे थे । वह इतनी शांति से और आराम से अपनी बात कहे जा रहे थे कि हमारे लिए बातों के तथ्य का वजन समझ पाना मुश्किल था । लेकिन, बस इतने तक । जरा देर हम टकटकी लगाए होंगे कि उनका पारा चढ़ गया ।
–खच्चर बेहूदा सब कहीं का! जयंती मनाएंगे! इतना जूता मारेंगे कि मारेंगे दस तो गिनेंगे एक । भागते हो कि नहीं ?
–जी बाबा, हमलोग जाते हैं । आप शांत होइए ।
–रे, वो तो चोट्टा मर गया कि इस गांव का पाप टला! अभी तक अगर जिंदा रहता तो गांव का धर्म नहीं बचता–––जयंती मनाएंगे! हम जाते हैं सबके बाप को ‘परचारने’–––
इतनी बात तो हमने आधी सुनी, आधी सुनी भी नहीं, तेजी से भाग खड़े हुए । उस दिन, बातों बातों में यह बात चर्चा में आ गई । मैं गांव में था और केदार (कानन) आए थे । साथ में थे–सुभाष (चंद्र यादव) भाई, सुस्मिता (पाठक) जी, रमण (कुमार सिंह) और प्रभात (झा) । मेरे ये सभी आत्मीय मेरे गांव, मेरे घर आते रहते हैं । लेकिन, इस बार का आना अलग था । केदार बरसों से बोलते थे कि राजकमल का घर आंगन देखने जाना है । मैं टालता था । दुख को जितना टालो, अच्छा होता है । राजकमल का घर देखेंगे तो क्या होगा ? दुख होगा । संताप से भर जाएंगे आप । पीड़ा होगी कि मरने के इतने बरस बाद भी उन्हें माफ नहीं किया गया । कोफ्त होगी कि लोग राजकमल का सगा प्रियपात्र बता बताकर आपका भेजा खा जाएंगे । आप गहरे अफसोस में डूबेंगे । आंखें भर आएंगी । ‘नोर’ टपक पड़ेंगे। मित्र हूं तो इतनी तकलीफ में क्यों पड़ने दूं आपको ?
लेकिन, केदार ने इस बार जबर्दस्त जिद पकड़ी थी ।
हम राजकमल का घर देखने गए । घर नहीं था । हमें मालूम था कि घर अब नहीं है । नहीं मतलब बिल्कुल नहीं । वहां मिट्टी थी । जंगल झाड़ उगे हुए थे । पड़ोसियों ने खर पतवार जमा कर रखे थे।
पपीते के गाछ पर तिलकोर, पनझोर, सपेता और न जाने कौन कौन सी लत्तियां लतरी हुई थीं । वहां घर नहीं था । वह जमीन अब राजकमल के हिस्से में रही भी नहीं । नीलू को किसी दूसरी जगह हिस्सा मिला, यहां नहीं मिला । यहां धीर बाबू और सुधीर बाबू के बच्चों का हिस्सा है । घर नहीं है, केवल स्मृतियां हैं, ताकि केदार जैसा कोई साहित्यकार कभी कभार टपक आए तो रोकर जाए । दस बरस से भी ज्यादा हुए । मुझे मालूम था कि घर अब नहीं है । घर नहीं, बंगला । इसे हम फूलबाबू का बंगला कहते थे । मिथिला के बौद्धिक लोग इसे ‘कवि कुटीर’ कहते थे । मालूम था । लोगों को मालूम है कि महिषी के पूरब धेमुड़ा बहती है और पच्छिम कोशी । मगर कितने लोग जा जाकर सत्यापन किया करते हैं ? कभी देख लिया, बस । दिमाग में उसका चित्र बना रहता है । आगे कभी
पता चले कि धेमुड़ा की धारा अब सूख चली तो दिमाग के चित्र में बहते पानी को हम सुखा लेते हैं । सत्यापन कौन करने जाता है ? पचास तरह की झंझटों का नाम जीवन है । घर अब नहीं है, यह भी कोई सत्यापन की बात हुई ? हां, यदि यह पता चला होता कि बुधवारयवालों ने या किन्हीं और ने हीे राजकमल की ‘डीह’ पर स्मारक बनाया है तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी । अच्छी तरह से पता था कि घर अब नहीं है । लेकिन घर नहीं तो आखिर क्या है, यह देखने
दिखाने जब गया, तो जो हालत हुई उसकी बात पूछिए ही मत! और, मधुसूदन बाबू की हवेली को देखते–देखते जो हुआ, वह तो और भी मत पूछिए । मैं कोई अकेला नहीं था साहब, सबकी आंखें भर आई थीं।–––और, भरे दिल से दिन भर ‘बदरिकाश्रम’ में बैठकर हम उन पुराने किस्सों को याद करते रहे थे ।
वे दिन थे कि जब राजकमल चौधरी को गुजरे बारह बरस बीत चुके थे । और, कोशी में जाने कितना
सारा पानी बह चुका था, और उसके साथ जमीनें भी । और, देवी तारा की बलि वेदी पर बीसियों हजार छागों की बलि दी जा चुकी थी । तीन चार बार अकाल पड़ चुका था, पांच छह बार अगलगी हो चुकी थी । सींकिया सामंतों की एक पीढ़ी तो गुजर गई थी, मगर ऐसे ढेर सारे नए लोग पूरी चमक में थे जो बातों के बम से संसद भवन को भी धराशायी कर सकते थे । यह राजकमल का गांव, महिषी था, जहां अब तक भी न तो सड़क पहुंची थी, न बिजली । गरीबी और बदहाली बदस्तूर कायम थी । साल दर साल कोशी की छाड़न उफनती और अगले एक साल तक रोते रहने का सौगात दे जाती । लोग फिर भी सहज जीवन जीते, भांग और गांजा और ताड़ी के भीतर से निकलनेवाले रास्तों में सुकून की तलाश करते पाए जाते थे । सुकून देने के लिए बहुत बड़ी ताकत मौजूद थी । वह थीं–देवी तारा, जिनके बारे में राजकमल कहा करते कि तेरह हजार साल पहले मेरुदंड पर्वत की काली चट्टानों से तराश ली गई तेरह साल की लड़की थीं वह, जबकि वह उग्र भी नहीं थीं, तारा भी नहीं, उनके लिए महज उग्रतारा थीं । लोग थे कि ये उलझन भरी बातें नहीं समझते थे, मगर वह उग्रतारा उनके लिए भी वही उग्रतारा थीं । और, वे दिन थे कि जब कोशी के इस पर्यावरण में हमारी आंखें खुल रही थीं । धीरे धीरे हम
उस लायक हो रहे थे कि आदमी जिन्हें देखता है, उन्हें उनकी असलियत में जानना चाहता है । हर चीज के लिए एक आतुर जिज्ञासा । हर बात के भीतर से उभरती ढेर सारी नई बातें और प्रश्न––– । प्रश्न ढेर सारे थे मगर उनके ठीक ठीक उत्तर, जो हमें संतुष्ट कर सकें, दे सकनेवाले लोग नदारद थे । उपस्थितों से यदि काम न चले तो लोग अनुपस्थितों की तरफ मुखातिब होते हैं, और इसी दौरान उसकी मुलाकात ‘साहित्य’ नामक फेनोमेना से होती है । हमारी तो ऐसे ही मुलाकात हुई
थी । गुलशन नंदा और कर्नल रंजीत पढ़ते पढ़ते कब हम प्रेमचंद और हरिमोहन झा और विमल मित्र
के पास पहुंच गए, हमें भी पता न चला था । और, ये ही वे दिन थे कि जब हमने राजकमल चौधरी का आविष्कार किया था।
संपर्क :
तारानंद वियोगी
मोबाइल – 09431413125
ईमेल – tara.viyogi@gmail.com