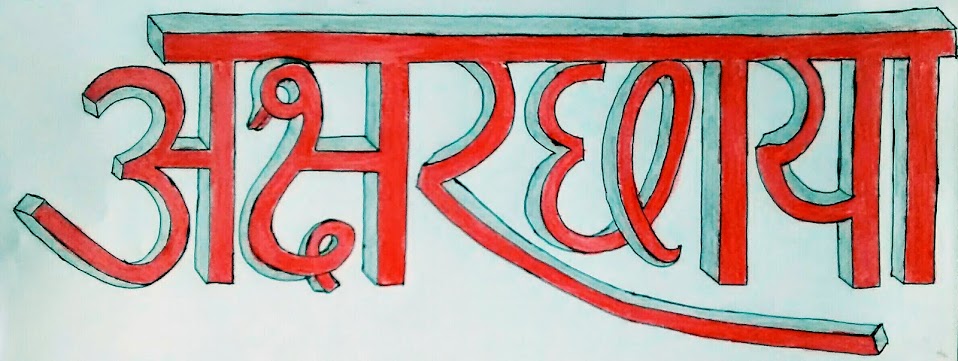किसी रचनाकार की कृतियों से परिचित होने के पश्चात पाठकों में एक सहज कुतूहल जगता है कि इस कृति के पीछे यानी इसकी सृजन-प्रक्रिया में रचनाकार किन परिस्थितियों से रूबरू था...उन हालातों ने उसे कैसे रचना के लिए प्रेरित किया। किसी मौलिक रचनाकार के पास इन सब सवालों के स्पष्ट जवाब होते हैं। ऐसे ही रचनाकार की रचना-प्रक्रिया को जानने का अवसर मिला...खुद रचनाकार की जुबानी। तो अवगत होते हैं...कहानीकार संदीप मील की लंबी कहानी 'कोकिलाशास्त्र' की रचना प्रक्रिया से।

संकटों से उपजी कोकिलाशास्त्र

'कोकिलाशास्त्र' मेरी दूसरी लंबी कहानी थी, इससे पूर्व मैं 'दूजी मीरा' नामक एक लंबी कहानी लिख चुका था। इनके अलावा अभी तक मेरा छोटी कहानियाँ लिखने का ही अभ्यास था। इस स्तर पर कहानी की संरचना को व्यवस्थित गति से / धैर्यपूर्वक निभाना मेरे लिये एक चुनौती थी। लेकिन अभी तक मैंने यह तय नहीं किया था कि कोई बड़ी कहानी लिखकर इस चुनौती का मुकाबला करुं।
जब 'कोकिलाशास्त्र' के लिखने की शुरुआत हुई, तब मैं जयपुर में एक किराये के कमरे में रहता था। आर्थिक तंगी का दौर था, उस दिन जेब भी खाली थी और रसोई भी। यह तो मैंने बाद में तय किया था कि पैसा आते ही सबसे पहले पर्याप्त मात्र में आटा खरीद लिया जाए और मकान मालिक को किराया दे दिया जाए। उसके बाद का महीना खाली जेब के निकालने में संघर्ष की एक उम्मीद तो बनती ही है। कमरे में देखा तो सारी रद्दी पहले ही बेची जा चुकी थी। किताबें बेचकर आटा लाना कोई नई बात नहीं थी क्योंकि मेरी कुल चल–अचल संपत्ति किताबें ही हुआ करती थीं। वैसे भी एक रचनाकार के पास मिल ही क्या सकता है इनके सिवा।
अब दूसरे विकल्प के तौर पर यह बचा था कि किसी से उधार ले लिया जाये। इस पर बहुत देर तक चिंतन करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि इस इलाके के जितने परिचित थे उन सबका पहले से ही कर्ज़दार था। वे इंतज़ार करते थे कि कब करार पर मेरी जेब में पैसे हों और उनका नसीब खुले।
जब कहीं कोई आशा ना दिखी, तब पिछले दिनों खरीदकर लाई पत्रिकाओं को पलटने लगा। हाँ, यह जरूर तय था कि शाम तक कुछ न कुछ व्यवस्था हो जायेगी। अगर कुछ भी नहीं हुआ, तो घर जाना पड़ेगा। वहाँ से आटा ले आयेंगे। पत्रिकाओं को पलटने के दौरान मेरी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी जो 'कथादेश' नामक पत्रिका में प्रकाशित था। इश्तिहार ऐसा था कि कोई विदेशी कम्पनी कथादेश के साथ मिलकर एक 'रहस्य–रोमांस कहानी प्रतियोगिता' का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता की एक विशेष बात यह थी कि विजेताओं को पच्चीस हजार रुपये भी मिलने तय थे। यह बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वक़्त मुझे पैसे की सख़्त ज़रूरत थी। इश्तिहार पढ़ते ही पत्रिका को बिस्तर के एक किनारे पर रखा और कहानी लिखना शुरु कर दिया।
चूंकि लिखने बैठ ही गया था, तो किसी किस्से की छोटी–सी डोर पकड़कर पार उतरना था। किस्से अपने पास जो थे, सारे के सारे स्मृतियों के खजाने में बंद थे। सबसे पहले यादों के दरवाज़े खोले, कई किस्सों ने अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराई। लेकिन कोई किस्सा जम ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे दिमाग पर प्रतियोगिता की एक शर्त सवार थी, किस्से में ‘रहस्य और रोमांस’ होना चाहिए। स्मृतियाँ लगातार कई ऐसे किस्से खोजकर ला रही थी जिनमें बहुतायत में ‘रहस्य’ थे। सिर्फ उन कहानियों में ‘रोमांस’ भरना था। मेरी सारी स्मृतियाँ लोक पर आधारित थी। यह काम बड़ा आसान होता है किसी भी रचनाकार के लिए कि वे लोक की कोई कहानी उठाकर उसके ढ़ाँचे में नये भावों की अभिव्यक्ति करे। ऐसा काफी लोगों ने किया भी है और बाद में उसी को अपना ‘सृजन’ घोषित किया जाता है ।
मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे लिये कोई भी ‘रहस्य’ यथार्थ से दूर नहीं हो सकता। मुझे लगा कि जो मेरी स्मृतियों में ‘रहस्य’ के नाम पर जमा है, असल में वे चीजे़ं रहस्य ना होकर संसार का ‘अमूर्तीकरण’ है। इनका किसी प्रकार का तार्किक विवेचन नहीं किया जा सकता। तो फिर ये स्मृतियाँ आयी कहाँ से हैं ?
मुझे यह समझ में आया कि ये स्मृतियाँ मेरे बचपन की हैं, जब परिवार के लोग ऐसे ‘रहस्यों’ से मेरे दिमाग को व्यस्त कर देते थे जिन पर तर्क करना एक गुनाह माना जाता। इसलिये आप इन ‘रहस्यों’ को मानवीय स्वभाव पर पाबंदी लगाने के रूप में देख सकते हैं जो भय और भौतिक जगत के प्रति विरक्ति पैदा करते हों। यही इन रहस्यों की राजनीति है।
तो साब, मुझे ‘रहस्य और रोमांस’ पर एक कहानी लिखनी थी, जिससे कुछ पैसे मिलने थे और आप तो जानते ही हैं कि पैसों की मुझे सख़्त जरूरत रहती है। मैंने यह सोचना शुरु कर दिया था कि क्या कोई ‘वैज्ञानिक रहस्य’ भी होते हैं या फिर इन तथाकथित रहस्यों का कोई वैज्ञानिक अवलोकन किया जा सकता है। आप यह सोच रहे होंगे कि जो आदमी ज़िंदगी के हर मसले पर इतना उतावला हो, वह कहानी लिखने के दौरान इतना सोच कैसे सकता है ? आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं फुर्सत और सुकून में कहानी लिखने के दौरान ही होता हूँ। इस समय कोई चोर मेरा पूरा घर, जिस घर में आटा ना सही, किताबें तो होती हैं, उसको भी समेटकर ले जाये, तब भी कहानी को बीच में छोड़ना मुमकिन नहीं हो सकता।
एक स्मृति बार–बार चेतना के दरवाज़े पर दस्तक दे रही थी जो इतनी धुंधली थी कि उसका एक ही तार समझ में आ रहा था। वह तार यह था कि इंसान कभी जानवरों की भाषा समझता था। यह एक पुरानी लोक कथा का हिस्सा था जो सिर्फ इतनी लाइन में याद था। मुझे इस सूत्र में बहुत ताकत लगी। इस कहानी को जानने का प्रयास करना बहुत जरूरी था। गांव के दो–चार बुजुर्गों को फोन करके यह लोक कथा जाननी चाही लेकिन वे इससे अपरिचित थे। फिर मुझे अचानक यह याद आया कि किस्सा तो मेरी परनानी सुनाया करती थी और उस पीढ़ी का कोई बचा ही नहीं है। उसके बाद वाली पीढ़ी के कुछ लोग जरूर हैं लेकिन वे उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि उनकी स्मृतियां साथ नहीं दे रही हैं।
इसी उधेड़बुन में शाम को जयपुर के रचनाकारों से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि उस इश्तिहार की बात तो यहां के रचनाकारों की पूरी ज़मात में फैली हुई है। कई इस प्रतियोगिता के लिए कहानियाँ लिखने का मन बना चुके हैं और कइयों ने तो कथ्य भी तय कर लिए थे। वे अपने कथ्यों को ऐसे छुपा रहे थे जैसे कि उनकी जबां से एक लाइन फिसली कि सामने वाला उनके ज़हन में घुसकर पूरा किस्सा निकाल ले जायेगा। जबकि वे यह भी जानना चाह रहे थे बाकी लोगों के ख़्याल क्या हैं क्योंकि उन्हें ख़्याल टकराने का भी डर था। तो सारे लोग बातों को घूमा फिराकर कुछ तलाश कर रहे थे।
चूँकि मेरे पास कोई मुक़्कमल ख़्याल था ही नहीं तो चुराये जाने का सवाल ही नहींं उठता। वैसे भी, मेरा यकीन है कि वो ख़्याल किस काम का जो चोरी हो जाये। मैंने सबके साथ साझा किया लेकिन इस पर कोई सार्थक बात नहीं हो पाई क्योंकि एक तो मैं ख़ुद भी स्पष्ट नहीं था कि आख़िर यह ख़्याल है क्या। दूसरा यह था कि मेरे ज़हन में जो चल रहा था, वो अभी इस हालत में था कि उसे ठीक से बयां भी नहीं किया जा सकता।
रात को घर आ गया और आपको यह बताते हुये बड़ी खुशी हो रही है कि उस रोज़ यूँ ही बेमतलब एटीएम चैक किया, यह जानते हुये कि यह अपनी आदत के मुताबिक पन्द्रह रुपये बैलेंस होने की जानकारी देकर मेरा मज़ाक उड़ायेगा। लेकिन अफसोस तो तब हुआ जब उस एटीएम ने मुझे एक हज़ार रुपये बैलेंस बताया और खुशी-खुशी दो पाँच सौ के नोट पकड़ा दिये । जीवन में पहली बार इस मशीन के प्रति मोहब्बत जैसा कुछ अहसास हुआ। एटीएम से बाहर आया तो एक बार अमीरी जैसा भाव मन में आया क्योंकि जेब में एक हज़ार रुपये थे और ज़हन में एक बिना लिखी हुई कहानी थी।
मैं यह सोच रहा था कि ये पैसे कहाँ से आये होंगे ? अब ऐसा नेक दिल कोई दोस्त ही नहीं था जो कहते ही खाते में धन डाल दे, इसलिये दोस्तों से कहना ही बंद कर दिया था। ऐसा याद आ रहा था कि पिछले दिनों एक पत्रिका के लिये कहानी लिखी थी, हो न हो पैसे उसे ही भेजे हों।
रात गहरा चुकी थी और इस समय आटा अगर खरीद भी लिया जाता तो भी ज़ाहिर तौर पर मेरे से रोटियाँ तो बनने से रहीं। खाना होटल पर ही खाया। बिस्तर पर सोकर वापस कहानी बुनने में लग गया। यह तो दिमाग ने अब तय कर लिया था कि इसी कथ्य पर कहानी लिखनी है। भरा पेट बहुत जल्दी निर्णय ले पाता है, भूखे पेट की बजाय। मसला यहाँ फंस रहा था कि क्या इंसान ने कभी जानवरों की भाषा की डिकोडिंग की है ?
सुबह उठते ही इसी सवाल को लेकर विश्वविद्यालय जाकर एक विज्ञान के विद्यार्थी से सलाह मांगी। उसने यह बताया कि एक बार ऐसे ही किसी काम पर एक नोबल पुरस्कार मिला था। मेरे दिल को कुछ राहत मिली। वह विद्यार्थी यह वादा करके गया कि आप कैंटिन में दोपहर तक इंतज़ार कीजिए, मैं पूरी जानकारी लेकर आता हूँ ।
कैंटीन में कुछ साथी हरदम वहाँ बैठ रहते हैं और बेमतलब वाली गप्पें हाँकते रहते हैं जिनका भी कोई मतलब होता है। मैं आज उनके साथ नहीं बैठना चाहता था, कहानी के लिए एकांत की जरूरत महसूस की गई। कैंटीन के पीछे एक पानी की टंकी है जिसके बगल में पेड़ की गहरी छाँव रहती है। मैं वहीं बैठकर सोचने लगा। अब मुझे यह लग रहा था कि जिस समय में मैं जी रहा हूँ उसके क्या–क्या सवाल हैं ? हिंसा, भेदभाव, बेइंतिहा पर्यावरण के दोहन जैसे कई सवाल उभरे। सोचा कि इनमें से किसी एक को केंद्र बनाकर कहानी लिखी जायेगी लेकिन इन सबको अलग करके देखना मेरे लिये मुश्किल काम लग रहा था। सारे अंतर्गूंफित थे। यह तय किया गया कि किस्सा अपने हिसाब से ही चले तो ज्यादा बेहतर हैै उसे किन्हीं खाँचों में कैद कर दिया जायेगा तो वह किस्सा कम, भाषण ज्यादा हो जायेगा।
एक एक्टिविस्ट होेने के नाते यह भाषण वाला संकट भी कई कहानियों की रचना प्रक्रिया में आता रहता है। पता ही नहीं चलता कि कब कथाकार की जगह एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने ले ली। यह अंतर्द्वंद्व बड़ा ही मुश्किल होता है लेकिन फायदेमंद भी होता है। मुश्किल इन अर्थों में होता है कि हर पल सर्तक रहना पड़ता है कि एक लेखक के तौर पर ही किरदारों से सलूक किया जाये, राजनीतिक कार्यकर्ता कई बार किरदारों से संवाद खुद बेालने लगता है। यह नहीं समझ में आता कि कौन–सा संवाद किरदार का है और कौन–सा लेखक के हमजाद एक्टिविस्ट का।
फायदेमंद इन अर्थों में होता है कि यह एक्टिविस्ट की चेतना हमेशा लेखक को राजनीतिक रूप से सही करती रहती है। जब भी लेखक फंतासी के भंवर में फंसकर कोई तर्कहीन बात करता है तो उसके अंदर का एक्टिविस्ट कॉलर पकड़कर धड़ाम से यथार्थ के धरातल पर पटक देता है। थोड़े दिनों बाद में ये एक दूसरे के दोस्त भी हो जाते हैं। जैसे कि लेखक कोई कहानी लिखते वक्त पेंच में फँस गया, वह तुरंत उस एक्टिविस्ट को याद करेगा। कुछ देर तो वह नखरे दिखायेगा कि नहीं चला न मेरे बिना काम। बहुत अकड़ते थे। अंततः वह सुलह कर लेता और लेखक को राजनीतिक तौर पर बजा लेता। ठीक ऐसे ही उस एक्टिविस्ट के लेखक भी काम आता है। सृजनात्मक स्तर पर इतना काम आता है कि उसके हर भाषण की भाषा लेखक ही होती है।
इतने में वह विज्ञान का विद्यार्थी आता दिखाई दिया जिसके हाथ में एक किताब थी । बहुत मोटी किताब थी जो नोबल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों के शोधों के बारे में थी। उसने एक पन्ना मोड़ रखाा था, वहीं से किताब खोलकर मुझे पकड़ा दी।
वैज्ञानिक का नाम था कार्ल वॉन फ्रिस्च और वह ऑस्टिया का निवासी था। फ्रिस्च को सन् 1973 में नोबल पुरस्कार मिला था। उन्होंने मधुमक्खियों के संवेदी धारणा पर शोध किया था और इन संवेदी धारणाओं को उन्होंने डिकोड करके अर्थ निकाले थे जोे उनकी किताब 'द डांसिंग बीस' में दर्ज़ हैं। अब मुझे एक ठोस प्रमाण मिल गया था कि एक वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा समझी है तो इंसान ऐसा कर सकता है।
शाम को कमरे पर आते ही कहानी शुरु हो गई थी। कहानी में एक चुनौती पात्रों के नामकरण की आती है। मेरी कहानियों के पात्रों के नाम बड़े आर्कषक नहीं होते, ऐसा कुछ मित्रों का मानना है। मुझे भी लगता है कि जब भी किसी पात्र का नाम रखना होता है तो मेरे ज़हन से नामों की फेहरिस्त ही ग़ायब हो जाती है। कोशिश के बाद भी मित्रों की भाषा में कहुँ तो ‘कोई ढ़ंग का नाम’ ना मिलता है तो कोई भी सामान्य नाम रख दिया जाता है। इसलिये पात्रों के नामों में एक तरह का रुखापन जरूर रहता है लेकिन क्या करुँ मेरे आसपास कोई तड़क–भड़क वाले नाम के लोग ही नहीं रहते हैं, वही मुरारी, शकील, सरिता, फातिमा नामों को जानता हूँ।
तो कहानी की मुख्य किरकार जो थी उसका नाम सरिता रखा गया। आधी कहानी लिखने के बाद वो प्रतियोगिता वाली शर्त याद आयी कि कहानी में रोमांस और रहस्य होना चाहिए। अचानक कलम रुक गई और सोचने लगा कि रहस्य तो इसमें हो जायेगा लेकिन रोमांस नहीं हो पायेगा। तब एक बार कहानी को वापस पड़ने लगा, अहसास हुआ कि कहानी बन रही है अब इसके साथ रहस्य–रोमांस करना छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी, आज आटा आ चुका था तो निर्णय लेने में बहुत देर नहीं लगी।
हालांकि यह कहानी उस प्रतियोगिता में भेजी गई थी जहां इसे कुछ नहीं मिल पाया जबकि उसी दौरान जयपुर के एक मित्र द्वारा लिखी गई कहानी पच्चीस हज़ार रुपये हासिल करने में सफल रही। अब यह कहानी प्रतियोगिता के दायरे से बाहर जा चुकी थी। दूसरे दिन दोपहर तक इसका पहला ख़ाका खींचा जा चुका था। फिर काफी दिनों तक इसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं दूसरे अफसानों में मशगूल हो गया। एक दिन 'बया' पत्रिका के संपादक ने कहानी माँगी तो याद आई कि घर में एक कहानी तो पड़ी है। उस दिन कहानी को छपने के लिए भेजने से पूर्व एक बार पढ़ा तो अंत में इत्मिनान की सांस ली कि इतने दिनों बाद भी मुझे इसमें कुछ भी जोड़ने–घटाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बस, इतना लगा कि इसने मेरे अंदर कुछ जगह खाली कर दी है, जहाँ अब बरसात का पानी ठहरता है जिसमें बारह मास पक्षी बोलते हैं और मैं चुपचाप कलम लिए उनकी भाषा को डिकोड करता रहता हूँ। यही रोजग़ार चल रहा है।
संपर्क :
संदीप मील
मोबाइल – 09636036561
ईमेल –skmeel@gmail.com
ग्रा. पो. – पोसानी,
वाया – कूदन,
जिला – सीकर,
राजस्थान - 302031
संपर्क :
संदीप मील
मोबाइल – 09636036561
ईमेल –skmeel@gmail.com
ग्रा. पो. – पोसानी,
वाया – कूदन,
जिला – सीकर,
राजस्थान - 302031