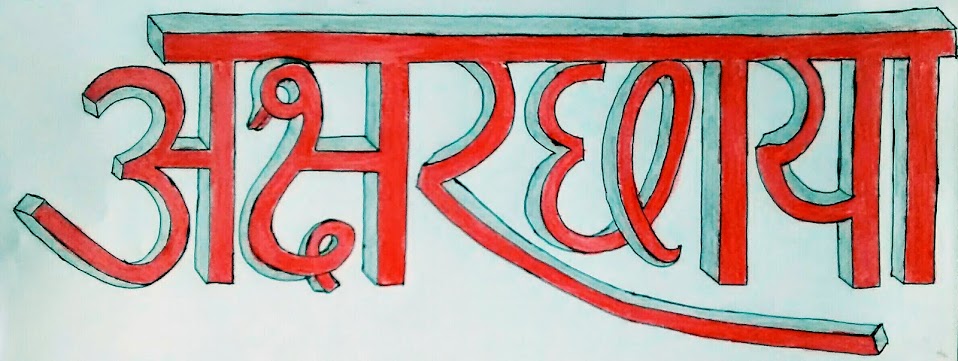दिव्या विजय का पहला कहानी-संग्रह ‘अलगोज़े की धुन पर’ पाठकों के बीच आ चुका है। पढ़ते हुए लगा कि उनकी कहानियों के पात्र अंतर्मन में उठते द्वंद्व पर इतने आत्म हो जाते हैं कि स्वसंवाद गहराता चला जाता है। इस संवाद प्रक्रिया में वे अपनी चेतना में और जीवंत हो उठते हैं बल्कि यह कहिये कि वे अपने अस्तित्व की अर्थवत्ता ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में कौन अपने को कितना पाता है...कितना छोड़ जाता है, इसे आप उनकी कहानी पढ़कर अनुभव कर सकते हैं। उनकी कहानियों का भाषा-शिल्प अपने सहज प्रवाह में पाठकों को कथ्य की गहराइयों तक ले जाता है, जिसकी अनुभूति लंबे समय तक बनी रहती है।
तो आइये पढ़ते हैं दिव्या विजय की नई कहानी।
पियरा गई बेला स्वंजन की...
दरवाज़े पर हल्की-सी दस्तक हुई। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के पश्चात पुरुष ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। अपनी उसी विशिष्ट शैली में। अंगुलियाँ घसीटते हुए दरवाज़े के बीचों-बीच अतिरिक्त दबाव देकर ज़ोर की रगड़। इस तरह कि जो स्वर हो उसे सिर्फ़ वही सुन सके जिसके लिए वह है। स्त्री जो भीतर थी वह सप्ताह-भर इसी आवाज़ की प्रतीक्षा करती थी। उसके सातों के सातों दिन के प्राण इस एक स्वर में अटके थे। जिस दिन यह आवाज़ आनी होती वह सारे काम निःशब्द निबटाती कि कहीं यह सरसराहट उसके कानों से अनसुनी न रह जाए। वह पाँव ज़मीन पर रखती तो इस तरह कि पाजेब के घुँघरू न बज उठें...हाथ उठाती तो इतनी मंथर गति से कि कंकण न गा उठें। वह दिन बुधवार का होता था। यूँ यह दिन सप्ताह में कभी अनायास भी आ जाता तो आवाज़ उसे उतना ही सजग पाती जितना बुधवार को। वह घर के किसी भी कोने में हो यह शब्द उसे अवश्य सुनायी देता। वह कहीं भी हो सकती थी...रसोई में बर्तन धोती हुई, कमरों की सफ़ाई करती हुई, पूजाघर में आरती उतारती हुई या बिस्तर पर अलसाई-सी परन्तु वह इनमें से कहीं नहीं होती थी। वह होती थी घर के सुदूर कोने में...ऊँची दीवारों से बने ओसारे में आसमान के नीचे नहाती हुई... वहाँ-जहाँ बाहर के स्वर नहीं पहुँचते परन्तु उसका मन दरवाज़े के निकट एक ताक में रखा रहता। ज्यों ही आवाज़ होती मन की डोर से बँधी साड़ी लपेटते हुए वह चली आती पर आज वो नहीं आयी।
वो हतप्रभ था कि वह आयी क्यों नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ...फिर आज क्यों। क्या भीतर वो अकेली नहीं है? हो सकता है उसका पति आज यहीं हो। उसका पति हर मंगलवार रात बाहर जाता था और गुरूवार अलसुबह लौट आता। इसीलिए पुरुष ने सप्ताह में मिलने वाली एक छुट्टी बुधवार को बाँध ली थी। वो रविवार के दिन भी काम पर जाता कि बुधवार का दिन उसके साथ बिता सके। उसकी पत्नी हैरान रहती कि यह कैसी नौकरी है जहाँ एक भी अवकाश नहीं मिलता। एक बुधवार का दिन अपने लिए रखने को उसे कई झूठ बोलने पड़ते। पर ये झूठ निरंतर दो वर्ष से सफल थे। पत्नी अभ्यस्त हो चली थी। बाक़ी के छः दिन पुरुष का अत्यधिक प्रेम उसके सारे संशय ख़त्म कर देता। इस तरह उस एक दिन की कसर पूरी हो जाती। प्रश्न यह उठता है कि क्या सचमुच वह अपनी पत्नी को प्रेम करता था? अगर करता था तो नए सम्बन्ध की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी। वह अपनी पत्नी को प्रेम करता था...कम-से-कम वह तो यही मानता था। तो उसके जीवन में यह जो मानने-भर का प्रेम था उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए वो नए प्रेम में पड़ा था। नया प्रेम किसी भी नयी वस्तु जैसा था। साफ़-सुथरा, चमकदार और सुन्दर। युवावस्था-सा अल्हड़ प्रेम पा वह भरा-भरा अनुभव करने लगा था। भरा होकर भी वह हल्का था। अब उसे कोई बात बुरी नहीं लगती...संसार उसे अपने प्रेम जितना ही आकर्षक लगने लगा था। तो अपने इसी प्रेम से मिलने के लिए उसने बहुत जुगाड़ लगाकर दफ्तर से बुधवार के अवकाश की व्यवस्था की थी। इतने बड़े झूठ को साधे रखना कठिन था और इस से भी दुःसाध्य था घर पर सबसे यह बात छिपा कर रख पाना। पर वो अच्छी तरह यह कर पा रहा था। प्रेम बहुत-सी असंभव लगने वाली बातों के लिए हिम्मत देता है।
पुरुष बुधवार को जल्दी जाग जाता था। उस दिन तैयार होने में वो पूरी सावधानी रखता। अपने शरीर का ध्यान रखने का उसे अभ्यास था पर उस दिन वो अधिक ध्यान देता कि उसकी वजह से स्त्री को कोई कष्ट न हो। उस दिन वो बालों को साबुन की बजाय शैम्पू से धोता और उन पर कड़वा तेल नहीं चुपड़ता था। औरत को उस तेल की गंध अप्रिय लगती थी। उस दिन वो कलफ़ लगे कुरते के स्थान पर साधारण इस्त्री किया कुरता पहनता। स्त्री को कलफ़ की महक भी पसंद नहीं थी। वह उस दिन घर से ज़रा जल्दी निकलता...स्त्री के लिए उपहार ख़रीदता, इत्र के फाहे लेकर कान के पीछे दबाता और ट्राम पकड़कर उसके घर के निकट वाले स्टेशन पर उतर जाता। स्त्री को उपहार का लोभ नहीं था। वह जानती थी पुरुष मेहनती है। हर सप्ताह उपहार ख़रीदना उसकी मेहनत का सदुपयोग वह कतई नहीं मानती थी। लेकिन स्त्री की इसी समझदारी को पुरुष पसंद करता था और अपनी औकात-भर एक सौगात वो उसके लिए अवश्य लेता। अगर औरत लालची होती तो वह ऐसा कदापि नहीं करता। पर वह हर सप्ताह उसे मीठी झिड़की देती, “तुम ये सब क्यों ले आते हो? हर बार ख़र्चा करने की ज़रुरत कहाँ होती है।” और उसके लाये उपहार को इतनी कोमलता से छू कर देखती कि वो निर्जीव चीज़ें भी सिहर कर रह जातीं। फिर उन्हें सहेज कर यूँ रख देती जैसे वह कुछ बहुत कीमती ले आया हो। उसके लाये उपहार में होता ही क्या...कभी एक्सपोर्ट शॉप से खरीदी छोटे-से डिफ़ेक्ट वाली चादर तो कभी थोक की दुकान से ख़रीदे दो एक-से कप। एक बार वो अख़बार की क़तरनों से उसके लिए नाव बना ले गया था। मस्तूलों वाली नाव जिसमें ढाँचे से लेकर नाव की पेंदी, पतवार तक..सब अख़बारी कागज़ से बने थे। उसे एकबारगी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कागज़ से बन सकता है। जब स्त्री ने उसे छुआ तो घर हैरानी भरी हँसी के कगार पर खड़ा था। अगली बार वो आया तो नाव काँच के घर में उपस्थित थी। स्त्री ने काँच पर लहरें उकेरी थीं और नाव उन लहरों पर रख दी थी। वो ख़ुशी से भर गया। यह स्त्री की ओर से पहली भेंट थी। इसके बाद भी स्त्री ने कई उपहार दिए।
एक बार वह उसके लिए कुम्हार के चाक पर जा एक सुराही बना लायी थी। स्त्री जानती थी कि गर्मियों में सुबह-सवेरे वह सुराही का पानी पसंद करता है। सुराही पर अद्भुत नक्काशी थी। स्त्री ने ऊँट पर भागते हुए ढोला-मारूँ उकेरे थे। ढोला पलट कर मारूँ की ओर देख रहा था और दोनों की दृष्टि एक-दूजे में बिंध कर रह गयी। एक बुधवार पुरुष नहीं आ सका था। उसे शहर से बाहर जाना था। स्त्री जानती थी मगर वियोग में अधीर हो उठी थी। दरवाज़े पर टँगे मन ने उस रोज़ अनेक बार उसे मरीचिका की ओर धकेला। शब्द की मरीचिका..उसे भान होता कि अभी कोई ध्वनि गूँजेगी। उसने अपने तमाम आभूषण उतार कर रख दिए..वस्त्र सरसराते थे तो उसने धारण किये वस्त्रों को त्याग दिया। उसने रसोईघर की ओर देखा भी नहीं कि बर्तनों का कोलाहल उसके जीवन के मादक स्वर को न निगल जाए। एक सप्ताह की प्रतीक्षा दुगुनी हो उठी थी। अगले बुधवार वो पहुँचा तो गले लगकर धीमी आवाज़ में स्त्री गुनगुना उठी..
आखडीया डम्बर भई, नयण गमाया रोय
क्यूँ साजण परदेस में, रह्या बिंडाणा होय
विरह अग्नि में जलती मारूँ ने यह गीत अपने दूत को सिखा कर भेजा था। मारूँ जो वर्षों से अपने प्रियतम द्वारा लिवा ले जाने की राह देख रही थी और प्रियतम था कि बाल्यावस्था की ब्याहता से अनभिज्ञ दूसरा ब्याह रचा बैठा था। प्रतीक्षा और प्रेम के इस आख्यान में अनिंद्य सुंदरी मारूँ के कोमल हाथों में आँसुओं से भीगे आँचल को निचोड़ते-निचोड़ते छाले हो गए थे। ऐसी दारुण प्रतीक्षा का अंत इसी गीत के कारणवश हुआ था। ढोला जो अपने शैशव की दुल्हन को बिसरा चुका था यह गीत सुन मारूँ को विदा कराने जा पहुँचा था। गीत में हिलोरें लेती पीड़ा सुन पुरुष की पलकें भीग आईं। उसने स्त्री को अंकवार भर लिया। उसके बाद कोई बुधवार नहीं था जब पुरुष न आया हो। अब पुरुष प्रायः यह गीत सुना करता। स्त्री की आवाज़ अत्यंत मधुर थी। वो रसोई में, आँगन में, छत पर..सब जगह गुनगुनाती। पुरुष की आकांक्षा पर वो बिस्तर पर भी गुनगुनाने लगी थी। रागों के आरोह-अवरोह उसकी देह की लय संग ताल मिलाते थे। पुरुष चकित रह जाता। स्त्री को पुरुष का विस्मय मोहता था। वो नित इस कला में प्रवीण होती जा रही थी। वो नए शब्द जोड़ती, उन्हें रागों में बाँधती...स्वरों को क्रम से रखते हुए हर स्वर पर उसकी घनी केशराशि की एक चुन्नट खुलती और देह के भीतर एक गिरह बढ़ती। देह के भीतरी अंग आपस में गुँथ जाते। निषाद तक पहुँचते-पहुँचते देह के भीतर की गिरह इतनी कस जाती कि चट से टूट जाती और केश सुलझ कर पुरुष को ढक देते। एक उसाँस दोनों के मुँह से निकलती। कुछेक क्षण का मौन रहता और स्त्री फिर सुर उठा लेती। इस बार स्वर अपने स्थान से नीचे खिसक कोमल हो जाते। मंद्र सप्तक में कोमल स्वर हृदय से रिस कर उसे तर कर देते। बाद में स्त्री ने गले का उपयोग बंद कर दिया। स्त्री ने देह के घर्षण से संगीत उत्पन्न करना सीख लिया था। पुरुष प्रेम में सिक्त था।
वो हर बार उसके आने पर वही चादर बिछाती जो वह ले आया था...जिस पर बड़े बड़े लाल गुलाब बने हुए थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन गुलाबों में केवड़े की महक आती। ऐसा नहीं था कि यह ख़ुशबू चादर को बरतने के बाद आने लगी थी। उसके इत्र के फाहों से इस महक का लेना-देना नहीं था। वस्तुतः वो उसके लिए तकियों के गिलाफ लेने गया था। स्त्री ने एक दिन बताया था कि उसे बैंजनी रंग के फूलों वाली बेल बेहद अच्छी लगती है। स्त्री के पास एक हरी चादर थी। पुरुष ने सोचा उसके ऊपर बैंजनी रंग के तकिये उसे फूलों का अनुभव देंगे। वहीं गिलाफ़ देखते हुए उसे केवड़े की तेज़ सुगंध आई। उसने अपना कान टटोला। नहीं, अभी इत्र लेना बाकी था। उसने अपने समीप देखा। एक औरत चादर देख रही थी मगर पसंद न आने पर बाहर चली गयी थी। चादर अब भी बिखरी पड़ी थी। लाल गुलाबों ने उसका मन मोह लिया। उसने चादर को छू कर देखा तो लगा जैसे मखमल को छू लिया हो। उसने चादर गाल से सटा ली तभी उसे पहली बार मालूम हुआ कि सुगंध का स्रोत चादर के भीतर कहीं है। उसने अपनी जेब टटोली, पैसे पूरे नहीं पड़े। उसने अपनी घड़ी के बदले चादर मोल ली थी। स्त्री उस से रूठ गयी थी। पुरुष ने चादर फैला दी...ख़ुशबू उन दोनों से लिपट गयी। स्त्री के अनमनेपन को अचम्भे ने आग़ोश में ले लिया। कई बार धोने के बाद भी चादर की ख़ुशबू नयी-नकोर थी। उनके प्रेम का बिछावन उनके प्रेम की भाँति ही मनोहर था।
दो बरस पहले दुर्गा-पूजा के पंडालों के भव्य दृश्य के मध्य पुरुष की निगाह स्त्री पर अटकी तो एकटक उसे ही देखता रह गया था। नवयौवना-सी...मगर नहीं...उसकी माँग में सिन्दूर बिखरा था। कैसा दग्ध कर देने वाला यौवन था...मटचिनिया चित्रकारी में प्रयुक्त होने वाले जले रंगों-सा। अवश्य नवविवाहिता होगी..उसकी नथ के पीले पत्थर पर उसकी आँखें स्थिर हो ठहर गयीं थीं। औचक वो हँसी तो उसकी धवल दन्त-पंक्ति से मंत्रबद्ध हो वह उसके पीछे-पीछे चल दिया। पीली साड़ी के लाल पाड़ को पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाये पर नहीं..यह तो उचित नहीं होगा। इस प्रचंड मस्तक के कीर्ति-क्षय का अधिकार उसे किसने दिया। यह उसकी और अपनी...दोनों की मर्यादा का उल्लंघन होगा। इतना असंयत वह कभी नहीं हुआ....थक कर वह प्रस्तर पर बैठ अपनी हथेलियों को रगड़ने लगा। आज उसकी सहधर्मिणी अस्वस्थ थी और हर वर्ष की भाँति महालया पर देवी के दर्शन पर आने को असमर्थ थी। उसी ने हठ कर उसे यहाँ भेजा था। क्या उसने देवी को पा लिया था। प्रतिमा से देवी निकल विचरण करती हैं क्या यह किंवदंती सत्य हो उठी थी।
नदी से सटे बाग़बाज़ार पंडाल में हज़ार हाथों से सैकड़ों राक्षसों का वध एक साथ करने वाली दुर्गा-मूर्ति विद्यमान थी। एकटक उस दिशा में देखते हुए उसकी आँखें अश्रुसिक्त हो उठी। उसने धुँधली आकृति देखी। एक ज्योति पाँत में बैठे भिक्षुकों को प्रसाद बाँट उनके आशीष से दीप्त हो उठी थी। स्त्री दुर्गा समान प्रतीत हो रही थी। उसकी आँखें चौंधिया गयीं। उसने अँगुलियों से मल कर आँखें खोलीं तो स्त्री प्रसाद बाँटते हुए उस तक आ पहुँची थी। न जाने किसकी प्रेरणा स्वरुप वह पत्थर से उठ खड़ा हुआ और घुटने मोड़ उसके आगे सर झुका दिया। स्त्री को अवाक् हो जाना चाहिए था...परन्तु स्त्री आगे बढ़ी और उसके सर पर हाथ रख ज्यों उसे वरदान दिया। पुरुष की आँखें बह चलीं। स्त्री क्षण-भर को उसके सामने ठहरी और विह्वल दृष्टि से उसे देखते हुए आगे बढ़ गयी। स्त्री की दृष्टि उसके मन को कोमल कर गयी। उसने देखा स्त्री की थाली का पोश वहीं गिर गया था। उसने उसे उठाया तो एक विद्युत् तरंग का आभास हुआ। वो रोमांचित हो उठा। स्त्री घाट की ओर बढ़ चली थी। नौका की प्रतीक्षा में वह अथाह जल-राशि को अपने केश से हिलोरे दे रही थी। शिथिल लहरें ज्यों उसे चूमने को उद्यत हो चली थीं। पुरुष ने नदी के तीर पर अपना स्पर्श रख छोड़ा जो बहते हुए जब स्त्री तक पहुँचा तो वह पलट कर बिहँस उठी। उसके मंद हास का अनुमोदन ज्यों अकस्मात आ पहुँची मेघ राशि ने भी किया। नौका आने में विलम्ब होता देख वह अस्त-व्यस्त हो उठी। पुरुष ने आँखों से उसे आश्वासन दिया तो वो अपनी लज्जा पार कर उस तक आई और हठीले स्वर में घर छोड़ देने का आग्रह कर बैठी। पुरुष उसकी आँखों और स्वर के विरोधाभास पर मुग्ध हो गया था। हाथी-दाँत युक्त हथफूल और स्वर्ण-जड़ित कंगन पहने उस कामिनी की कलाई थाम वो उसे उसके घर तक ले आया था।
बंगाली-मारवाड़ी परिवार की छोटी बहू से किसी को विशेष अपेक्षा नहीं थी। उसके अबोध स्वभाव के आगे सबकी सख़्ती नरम पड़ जाती। सब उसे पगली बहू बुलाते। पगली बहू रात गए तारे गिनती हुई खुले आँगन में नाच उठती। पगली बहू राजस्थान की मिटटी में पगी लोक-कथाएं सुन झर-झर रोती जाती। पगली बहू को घर की याद सताती तो कलकत्ते की हुगली को अपने गाँव का तालाब मान उसका जल पी जाती। पगली बहू पीली धूप को ललछौहें रंग में रंग कर मिटटी में दबा देती। पगली बहू चंपा और गुलचाँद की ख़ुशबुओं संग मह-मह महकती।
पगली बहू कितनी छोटी-सी थी जब अपने गाँव से उसका नाता टूट गया था। पहली बार अपने गाँव से दूसरे गाँव एक विवाह में गयी तो उसी मंडप में वह भी इस बंधन में बंध गयी। कैसी ख़ुशी कुलाँचे भर रही थी जब मालूम हुआ था कि ममेरी बहन के ब्याह में जाना है। कितने महीनों तक रंग-बिरंगे पत्थर बीनती रही थी कि वहाँ जाने पर सारे भाई-बहनों के साथ खेलेगी। माँ के साथ मिलकर सारे दुपट्टे नए सिरे से रंग डाले। माँ की साड़ियों से उसके लिए गोटेदार कुरते बनाये गए। झालरदार कुर्तियाँ कलफ़ लगाकर संदूक में बंद कर दी गयीं। माँ की नज़र बचाकर पड़ोस की सहेली से लाली माँग लायी कि ब्याह में ज़रा सजेगी-सँवरेगी। पिछले महीने दशहरे के मेले में ही तो उसे मालूम हुआ था कि होंठों को रंग कर खूबसूरत बनाया जा सकता है। एक थैले में किताबें भी भर ली थीं। जाने कितने दिन वहाँ बीत जाएँ। पढ़ाई थोड़े न छोड़ेगी, थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करती रहेगी जिस से लौटने पर अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण कर सके।
लेकिन फिर लौट कर कहाँ जा पायी? बरसों गुज़र गए। न वहाँ से बुलावा आया न यहाँ से किसी को याद आई कि उसका भी कोई घर था। यहाँ आई तो कुछ दिन रौनक रही थी। सब उसे छेड़ते और वह निष्कंप दृष्टि से सबको देखने के पश्चात शर्म और भय से सर झुका लेती। सब हँस देते। क्या होता था उस हँसी में..उपहास, स्वीकृति अथवा उदासीनता। पर अंत में उसने सब अंगीकार कर लिया था। यूँ भी कितने-से दिनों के लिए था यह मेला। सब भाई-बांधव दूर-दराज़ के शहरों में बसते थे। एक-एक कर सब लौट गए। सास-ससुर बचे। वो भी उसे गृहस्थी के तौर-तरीके समझा तीर्थ पर निकल गए। तब के जो निकले फिर वापस नहीं लौटे। कोई कहता रास्ते में ही मर-खप गए। कोई दबे स्वरों में कहता बेटे-बहू की मनमानी से घर छोड़कर वहीँ कुटिया बनाकर रहने लगे। पर यह बात इतनी दबे-छिपे स्वर में होती कि दीवारें भी अस्वीकार कर देती। पगली बहू क्या किसी को सताती। उसे तो मालूम ही न था कि सताना क्या होता है। पगली बहू का सांसारिक अनुभूतियों से सम्बन्ध ही नहीं था। पुरुष से प्रेम भी तो उसके लिए अलौकिक ही था।
स्त्री ने पुरुष का वरण क्यों किया? उसने कई बार विचारा पर कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। अपने घर-परिवार में वह तुष्ट दिखती थी। संभवतः उसकी प्रेम की आकांक्षा भी अतृप्त रही होगी। सुना तो था उसका पति उसे बहुत चाहता है। स्त्री स्वयं भी यही कहती। परन्तु एक बार वो हल्का-सा सुराग़ तब पा गया जब स्त्री प्रेम के मादक क्षणों में बुदबुदाई कि पुरुष उसका प्रथम प्रेम है। प्रथम प्रेम...प्रथम प्रेम...हाँ यही तो सुना उसने। प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने स्त्री को देखा तो वो फिर कुछ न बोली। कैसी रहस्यमयी थी वो! टप-टप आसमान बरसने लगा तो पुरुष को अपनी महीन दृष्टि से बाँध खिड़की तक ले गयी और सींखचो पर अपने आँचल का कोर बाँध न जाने कौन सी मन्नत माँगी। हफ़्तों तक आँचल परचम बना फहराता रहा। हवा संग आँचल सरसराता तो एक चुप-सी मुस्कराहट उसके होंठों पर खिल उठती। कुछ रोज़ बाद उसने देखा कि आँचल का टुकड़ा वहां नहीं है. क्या उसकी मन्नत पूरी हो गयी? उसे जिज्ञासा हुई। स्त्री ने उस दिन बहुत-से पकवान बनाये थे। धुले केश उसकी पीठ पर फैले थे और वो हर बार से अधिक गुनगुनाते हुए उसे खाना परोस रही थी। उसका भेद रह-रहकर उसकी देह के हर कोर से कम्पित हो उठता। क्या बात होगी? अंत में जब रहा नहीं गया तो वह पूछने को उद्यत हो उठा। उसके कुछ कहने से पहले ही उसने अपनी हथेली से उसका मुंह ढाँप दिया।
“पूछना मत. मैं ही कहूँगी। ”उसकी अँगुलियों से ऊर्जा पारित होती हुई उसके मन को आवेशित कर रही थी। उस दिन वह गौरैया-सी फुदकते हुए काम कर रही थी पर काम ख़त्म ही होने में नहीं आ रहा था। वो जितना उतावला हो रहा था स्त्री उसकी व्यग्रता में उतना ही आनंदित हो रही थी। वो बच्चों की भाँति मुँह फुला कर बैठ गया। स्त्री आई और उसके निकट धरती पर बैठ आड़ी-तिरछी लकीरें उसके पैरों पर खींचने लगी। उसे गुदगुदी हुई पर उसने नाराज़गी का भाव दिखाते हुए पैर खींच लिया। स्त्री ने फुसफुसाते हुए कहा, “हमारी सबसे बड़ी आकांक्षा याद है?”
पुरुष के मन में रात कौंधी और उदय होते सूर्य के रंगों के मध्य कौंधा उन दोनों का साथ।
स्त्री ने हँसते हुए हाँ कहा और उसके घुटनों पर सर रख दिया।
“उन्हें पंद्रह दिन के लिए बाहर जाना है। ”लजाती दृष्टि से स्त्री ने पुरुष को देखा। “तुम इन दिनों में कभी...” कहते-कहते उसकी आँखें और होंठ चंद्राकार में खिंच गए। होंठों का चाँद उसके सर पर एक चपत लगा कर कुलांचे भरता आसमान पर जा बिखरा। आँखों का चाँद पुरुष की आँखों में भी दीप्त हो उठा। एक नदी चाँदनी की दोनों के प्रेम में भीग गयी। अगली पंद्रह रातों ने सुख का आकाश रच दिया था। उनका प्रगाढ़ प्रेम निविड़ अंधकार के छींटों से और गहन हो उठा था। दिन के हर क्षण साथ रहने के सुख, कुछ घंटों के साथ के चितले सुख से कैसे भिन्न होता है यह जानकर दोनों विभोर थे। घर में वे दोनों थे पर कोई नहीं था। वे एक-दूसरे के भीतर थे...इतने भीतर कि उनकी उपस्थिति किसी को द्रष्टव्य नहीं थी परन्तु सारे घर को दोनों की उपस्थिति ने ढक लिया था। सुदृढ़ दीवारों से प्रेम का रिसाव होने लगा था। सुबह का सूरज दोनों की अनुमति से घर के भीतर प्रवेश करता था। सद्यःस्नात स्त्री की अलकों से चू आया जल उजास में लिपट कर इन्द्रधनुष रच देता।
वे दोनों अंतहीन बातें करते। पुरुष अपने दफ़्तर की बातें कहता..स्त्री अपने घर-परिवार की। पुरुष अपनी पत्नी की बातें कहता तो स्त्री कुतूहल से सुनती। पुरुष की गृहस्थी की बातें उसे दूसरे ग्रह की प्रतीत होतीं। वो कल्पना नहीं कर पाती कि उसके अतिरिक्त पुरुष किसी अन्य स्त्री के संपर्क में भी है। स्त्री के मन में स्त्री ही उसका विश्व थी। स्त्री छः दिन पुरुष में पगी घूमती। सातवें रोज़ पुरुष के साहचर्य को अपनी धोती के छोर पर बाँध लेती। पुरुष का संसार उसके संसार से किस प्रकार भिन्न है वो अनुमान नहीं लगा पाती। पुरुष उसके संसार को जानता था, उसे छू सकता था, उसका हिस्सा हो सकता था परन्तु वह इन सबसे अनभिज्ञ थी। पुरुष उसके तहख़ानों के रहस्य जानता था। वह उसके घर और उसके मन के भीतर के गलियारों से परिचित था। स्त्री उसके मन के पार उसके जीवन को भी परखना चाहती। पुरुष उसे सब कुछ बताता। अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या उससे बाँटता परन्तु स्त्री का मन नहीं भरता। उसे संतुष्टि नहीं होती। उसकी जिज्ञासा अथाह होती। बातों की असीमता से पुरुष को उकताहट नहीं होती वरन धीरे-धीरे उसे प्रतीत हुआ कि वह अपने घर और अर्धांगिनी को अपेक्षाकृत अधिक जानने लगा है। कितनी ही बातों की गुत्थियाँ स्त्री से बात करते हुए यूँ सुलझ जाती कि वह चमत्कृत रह जाता। घर का चित्रण करते हुए न जाने कब वो पत्नी के मन की भीतरी तहों के पार देखने लगा। मानने-भर का प्रेम असल प्रेम में परिवर्तित होने लगा।
इस बार घर लौटने पर अपनी पत्नी के केश गूँथते हुए उसे स्त्री का उज्जवल-धवल माथा याद अवश्य आता किन्तु वह चुम्बन अपनी पत्नी के माथे पर ही जड़ता। चुम्बन की समय-सीमा और दबाव बढ़ने लगा था। जो मिलता पत्नी उसे सूद समेत लौटा देती। वह सदा एक विशेष आभा से दमकने लगी थी। पुरुष उसे इस रूप में देख हतप्रभ था। स्त्री के जिस रूप का वह आकांक्षी था वह तो उसके इतना… इतना समीप था। स्त्री को सुनाते हुए वह स्वयं उस घर का हिस्सा हो गया जिसे वह अरसे से बिसरा बैठा था। अब पत्नी की बात करते हुए वह असम्पृक्त नहीं रहता वरन उसके स्वर में कोमलता घुल जाती। उसकी आँखें एक गोपन सुख से मुंद जाती। खोज का स्थान एक संतुष्टि ने ले लिया था जो उसके पोर-पोर से फूटने लगी थी।
यह क्या...स्त्री ने पहली बार लक्षित किया तो ईर्ष्या के भाव से घिर गयी। फिर पुरुष की आँखों में अपने घर को घटते हुए देखने लगी। उसके सम्बन्ध में अपने सम्बन्ध की परिणति खोजने लगी। पुरुष के मुख पर स्थिरता से उत्पन्न हुआ आकर्षण उसे विद्वेष से भर रहा था। क्या यह सत्य हो सकता है? क्यों...क्यों नहीं हो सकता। उसका अपना घर कहाँ है? वह तो पुरुष के साथ एक काल्पनिक स्थान पर बसर कर रही थी।
एक रोज़ पुरुष ने मिल के आगे से गुज़रते हुए नीले कंवलों के छापे वाली साड़ी देखी तो उसे लेने को मन कुनमुना उठा। स्त्री के पास तोहफ़ा लेकर पहुँचा तो स्त्री ने एक और पैकेट लक्षित किया। पुरुष ने मुस्कुराते हुए दोनों पैकेट उसे थमा दिए। एक पुरुष की अर्धांगिनी के लिए था। दूसरा उसके लिए, दोनों एक-से। स्त्री से कैसा दुराव...कितनी अपनी थी वह उसकी। स्त्री मुस्कुरा उठी और एक साड़ी उठाकर दूसरे कमरे में जा पहुँची। सम्पूर्ण शृंगार कर उसके सामने आई तो पुरुष एकटक उस मोहिनी को देखता रह गया। स्त्री ने उसे मन भर प्रेम किया और एक उदास मुस्कुराहट के साथ उसे विदा कर दिया।
और आज पुरुष फिर वहाँ था। उसी तरह दरवाज़े का अँगुलियों से चुम्बन लेता हुआ. वह प्रतीक्षा में था। परन्तु वह नहीं आई। क्यों नहीं आई? भला इतना विलम्ब! आज वह उस से झगड़ा करेगा। मानिनी नायिका की भाँति आचरण करेगा और इस विलम्ब के लिए तब तक उसे क्षमा नहीं करेगा जब तक स्त्री उसके लिए नया गीत नहीं रच देगी। वह इस कल्पना से भाव-विभोर हो उठा। उसने कान दरवाज़े से सटा दिए। उसे स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। एक और आवाज़ स्त्री की आवाज़ से सटी हुई थी।
“बहू जी, बाहर कोई है। कोई द्वार खटखटा रहा है। ”एक चौकन्नी आवाज़ कह रही थी।
ओह! आज उसकी सहायिका घर पर है. क्या वह उसे अवकाश देना भूल गयी?
“कोई नहीं है, तेरे कान बज रहे हैं। ”स्वर ने मिथ्या क्रोध दिखाया। फिर पुचकारते हुए कहा, “तू आलता लगा। अभी बहुत-से काम बाक़ी हैं। फिर उबटन भी मलना है।” कहते हुए एक गर्वीली मुस्कान शायद उसने फेंकी। पुरुष ने द्वार के समीप रखे मन को आवाज़ दी परंतु वहाँ कुछ नहीं था। मन तो आलते के रंगों में गमक रहा था। स्त्री ने पैरों में आलता लगाया था। अगले दिन उसके विवाह की वर्षगाँठ जो थी।
परिचय :
नाम - दिव्या विजय, जन्म - 20 नवम्बर, 1984, जन्म स्थान – अलवर, राजस्थान, शिक्षा - बायोटेक्नोलॉजी से स्नातक, सेल्स एंड मार्केटिंग में एम.बी.ए., ड्रामेटिक्स से स्नातकोत्तर
विधाएँ - कहानी, लेख, स्तंभ
‘अलगोज़े की धुन पर’ कहानियों की पहली किताब। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं जैसे नवभारत टाइम्स, कथादेश, इंद्रप्रस्थ भारती, पूर्वग्रह, जनपथ, नया ज्ञानोदय आदि में नियमित प्रकाशन। इंटरनेट पर हिन्दी की अग्रणी वेबसाइट्स पर अद्यतन विषयों पर लेख। रविवार डाइजेस्ट में नियमित स्तंभ।
अभिनय : अंधा युग, नटी बिनोदिनी, किंग लियर, सारी रात, वीकेंड आदि नाटकों में अभिनय। रेडियो नाटकों में स्वर अभिनय।
सम्मान - मैन्यूस्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट विनर, मुंबई लिट-ओ-फ़ैस्ट 2017
सम्प्रति - स्वंतत्र लेखन, वॉयस ओवर आर्टिस्ट
ईमेल- divya_vijay2011@yahoo.com