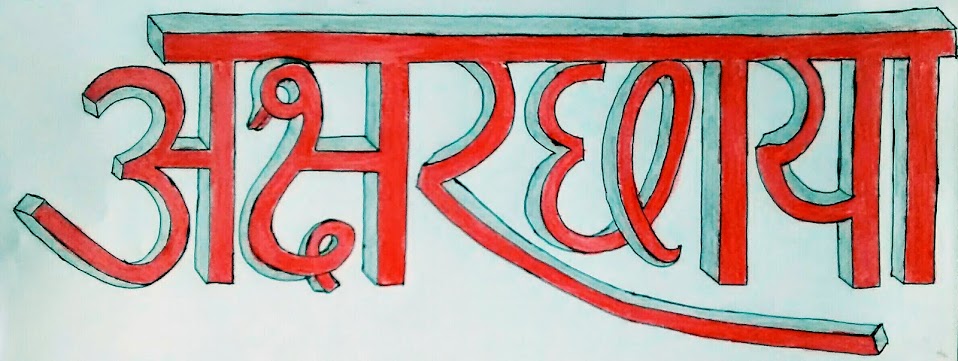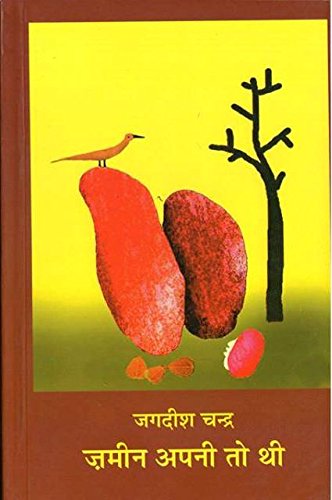दिव्या विजय मानती हैं कि अपने समकालिकों को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि समकालीन साहित्य सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। सामाजिक परिवर्तनों के साहित्य में दर्ज़ होने तथा साहित्य पर पड़नेवाले उसके प्रभाव के संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी है। समकालीन साहित्य को ये परिवर्तन भाषा-शिल्प एवं वैचारिकी के स्तर पर किस तरह प्रभावित करते हैं? इन परिवर्तनों के कारण मनुष्य में आये बदलाव को दर्ज़ करने में लेखक अपने बैकग्राउंड के कारण कैसे चूक जाता है… जहाँ वह अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकता था। आइये बात करते हैं।
नरेन्द्र कुमार : एक लेखक के लिए अपने समकालिकों को पढ़ना कितना जरुरी है?
दिव्या विजय : कल-आज के संयोग से ही तो सृजनात्मक चेतना निर्मित होती है और समकालीन साहित्य सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे न पढ़ना तो वर्तमान से मुख मोड़ने जैसा है। अतः समकालिकों को पढ़ने के लिए मैं उत्साहित रहती हूँ, अधुनातन प्रयोगों और नज़रियों को देखने की लालसा भी इसमें शामिल है। कई बार हम अपनी कुछ मानसिक आवश्यकताओं के प्रति अनभिज्ञ होते हैं और क्योंकि समकालीन साहित्य हमारे समय का प्रतिबिंब होता है इसलिए वे ज़रूरतें पढ़ने के दौरान स्वतः ही पूरी हो जाती हैं।
नरेन्द्र कुमार : आपकी दृष्टि में वे सामाजिक परिवर्तन कौन-से हैं जिनसे हमारा समाज दो-चार हो रहा है? क्या हिंदी साहित्य में इसे दर्ज़ किया जा रहा है?
दिव्या विजय : केवल दर्ज करने की बात कह कर तो हम साहित्यकार की रचनाशीलता को अनदेखा कर देते हैं। साहित्य में समाज को केवल सादृश्यता के आधार पर खोजने से अधिक सरलीकरण और क्या होगा? वह लेखन में समाज की पुनर्रचना करता है जिसमें न केवल उसका दृष्टिकोण बल्कि उसकी कल्पना और आकाक्षाएं भी शामिल होती हैं।
सामाजिक परिवर्तन अंतर्वस्तु के स्तर पर ही नहीं वरन् भाषिक स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, रूपादि के स्तर पर भी देखा जाता है। साहित्य क्योंकि वैश्विक दृष्टि को लेकर चलता है इसलिए परिवर्तनों को संज्ञा से अभिहित करने पर दृष्टि संकुचन का ख़तरा है। केवल अपने समाज में हो रहे बदलावों पर भी दृष्टिपात करें तो भी सबको समान बटखरों से कैसे तौला जाए।
नरेन्द्र कुमार : सामाजिक परिवर्तन भाषा, शिल्प एवं रूप के स्तर पर साहित्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
दिव्या विजय : साहित्य का ऐतिहासिक अनुशीलन करें तो आदि महाकाव्यों से ही समाज का प्रभाव भाषा, रूपादि पर गहरे दिखता है। इनका मूल रूप गेय और मौखिक था। यूनान में होमर के महाकाव्यों की स्थिति भी रामायण महाभारत जैसी ही थी। गण समाज में अवतारवाद और परलोकवाद की आवश्यकता की पूर्ति करते रामायण जैसे महाकाव्य कालिदास तक आते नाटक रूप ले लेते हैं जो नायकों के चार प्रकारों में ही बँधे रहते हैं और सामंती समाज से ही चुने जाते हैं। इस काल में विकसित लेखन संस्कृति में रचे गए, अलंकृत महाकाव्यों में कुलीन पात्रों तथा स्त्रियों और दासों की भाषा में अन्तर साहित्य निर्माण में वर्गीय मूल्यों के प्रभाव को ही दिखाता है। पश्चिम में ट्रेजेडी का आधार अभिजात्य वर्ग रहता था जबकि कॉमेडी में आम जन को स्थान मिलता था। यूनानी क्लासिकल रचनाओं के बरक्स शुरुआत में जो रोमन में लिखा गया और रोमान्स कहलाया, हेय माना जाता था परन्तु कालान्तर में समाज ने उसे भी क्लासिकल में ही गिना।
भक्तिकालीन 'अति मलीन वृषभानु कुमारी' रीतिकाल में आकर 'राधा नागरि सोई' हो जाती है। रीतिकालीन प्रशस्ति काव्य की भाषा आलंकारिकता से आक्रांत रही तो आधुनिक काल में पूर्ववर्ती भाषायें समाज के विचारों की वहन क्षमता ही खो बैठीं और खड़ी बोली सिरमौर हो गयी। इस भाषा ने अपने अनुरूप कितने ही साहित्यिक रूपों निबंध, उपन्यास, कहानी आदि का विकास कर लिया। मध्यवर्ग के महाकाव्य और आधुनिक चेतना के प्रतिनिधि साहित्यिक रूप उपन्यास ने तो नायक के लिए कभी कुलीन-अकुलीन का विचार ही न किया। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप शब्दों की अर्थवत्ता ही बदल गयी। स्वतंत्रता पूर्व 'नेता' शब्द क्या आज भी साहित्य में वही अर्थ रखता है?
नरेन्द्र कुमार : सामाजिक परिवर्तन जहाँ समाज को बदलता है, वहीं वह मनुष्य में भी बदलाव लाता है। मनुष्य में आये बदलाव को देखने में साहित्यकार की दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। साहित्यकार का अपना बैकग्राउंड यथा - जाति, वर्ग, नस्ल, जेंडर आदि उसकी दृष्टि को किस प्रकार प्रभावित करता है?
दिव्या विजय : साहित्यकार सामाजिक चेतना का वाहक बनता है परंतु उसकी दृष्टि सामाजिक यथार्थ पर भी होती है। कई बार वह बहुत आगे की यात्रा कर सामाजिक क्रांति तक भी पहुँचता है और कई बार उसकी दुविधा उसके पैर पीछे खींच लेती है। इसमें उसकी अपनी मान्यताएं, बैकग्राउंड, वर्ग इत्यादि उसकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं।
गुजराती भाषा में बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा 'सरस्वतीचंद्र'। समाज सुधार आन्दोलनों के प्रभाव में गोवर्धनराम त्रिपाठी ने इसमें विधवा विवाह के विषय को लिया और इसकी ख़ूब वकालत की। विधवाओं के प्रति सहानुभूति का स्वर रखते हुए इसे समाज की ज़रूरत बताया पर इतना सब कहने-लिखने पर भी वे उपन्यास के अंत में विधवा नायिका का विवाह नहीं दिखा पाए। ख़ासी आदर्शवादिता दिखा नायिका को त्याग की मूर्ति बना दिया। धार्मिकता, नैतिकता या वर्ग, कुछ तो था ही जो लेखक नारी से जुड़े सामाजिक सुधार को वैचारिक तौर पर तो स्वीकार कर पाया पर व्यावहारिक तौर पर नहीं। बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यासों और लेखों में भी विधवा विवाह के प्रति यह व्यावहारिक हिचक दिखती है।
लेखक की राजनैतिक पक्षधरता उसके साहित्य में राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति की विभाजन रेखा को अनदेखा भी कर सकती है। जाति-वर्ग तो क्या लेखक के रहने का स्थान भी उसके साहित्य को प्रभावित करता है। एक आलोचक ने कहा है कि प्रसाद ने कभी भी दोपहर का दृश्य नहीं लिखा और कहीं है भी तो सूचना-भर। कारण? वे बहुत तंग गली में रहते थे जहाँ आसमान की चीर भर दिखती थी। 'पथ के साथी' में महादेवी ने भी प्रसाद से मिलने उनके घर जाते समय गलियों को अजगर के उदर में घूमने जैसा बताया है। साहित्यकार में साहित्यिक वैचारिकता तथा जाति-धर्म आदि से चालित नैतिक व्यवहारिकता का द्वंद्व रहता है, जीत जिसकी भी हो साहित्य इससे अछूता नहीं।
नरेन्द्र कुमार : सामाजिक परिवर्तन समाज में नई चेतना लाने का काम करते हैं, जिसका प्रसार साहित्य के विभिन्न रूपबंधों के माध्यम से होता है। इस प्रकार साहित्य समाज में होनेवाले संभावित परिवर्तनों की भूमिका तैयार करता है। आप वर्तमान में साहित्य की इस भूमिका को किस तरह देखती हैं?
दिव्या विजय : साहित्य चेतना को जगाता है, संवेदना को माँजता है और जीवन को नयी दृष्टि भी प्रदान करता है। काल का अतिक्रमण कर आगामी परिवर्तनों की भूमिका तैयार करने की ज़िम्मेदारी तो साहित्य के पास हर काल में रहेगी यदि यह समाप्त हुई तो साहित्य की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। जेट स्पीड जेनरेशन में साहित्य की इस ज़िम्मेदारी के साथ इसकी चुनौतियों में भी इज़ाफ़ा हुआ है। माध्यमों की पहुँच ने जातीय साहित्य के बीच अलगाव मिटा कर उसे विश्व साहित्य बना दिया है। स्थानीय समाज के परिवर्तनों व समस्याओं के साथ विश्वदृष्टि और मूल्यबोध का प्रभाव भी उस पर है। बाज़ार में हर चीज़ के इंस्टैंट होने का दबाव साहित्य पर भी असर डाल रहा है, साहित्य सृजन के 'बरस बीते एक मुक्ता रूप को पकते' में पीछे छूट जाने का भय है तथा कलावादी हो या 'स्वांतः सुखाय' लेखन, पाठक की अपेक्षा तो है ही। कलात्मकता भी उत्पाद है और व्यक्ति के लिए वस्तु ही नहीं अपितु वस्तु के लिए व्यक्ति पैदा करने की शक्ति भी बाज़ार में है। ऐसे में बाज़ार के दबाव और सूचनाओं की बॉम्बार्डिंग के बीच साहित्य को ख़ुद को केवल इंद्रियोपजीवी बनने से बचाना होगा और सामाजिक विसंगतियों से आँख मिलाने का काम बदस्तूर जारी रखना होगा।