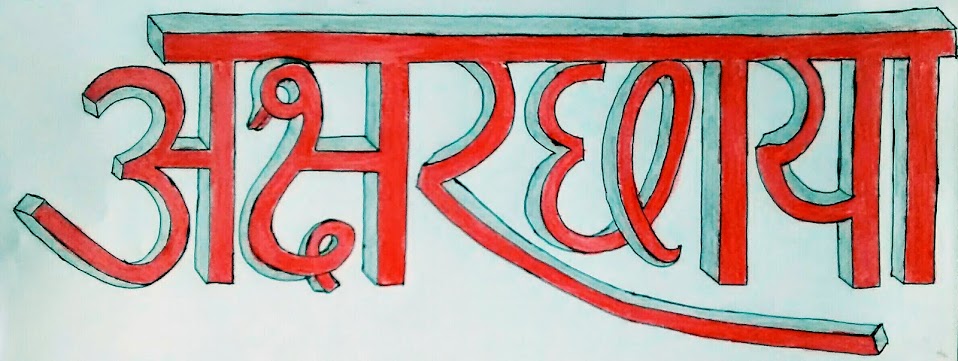दिव्या विजय ऐसी कथाकार हैं, जिनकी कहानियों की प्रतीक्षा पाठकों को रहती है। वह अपने लिए कोई फ्रेम तय नहीं करती… उन्हें यह भाता ही नहीं। पिछले वर्षों में ही अपने पहले कहानी-संग्रह ‘अलगोजे की धुन पर’ के उदात्त चरित्रों के मोह से आगे निकल जाने में उन्होंने देर नहीं की। वह आम भारतीय मन की ठीक-ठीक थाह लगाते हुए आगे बढ़ रही है। सफ़ेद-स्याह चरित्रों को लेकर बढ़ती हुई वह जैसे उनकी एक-एक मनःस्थिति पर गौर करती हैं। इसी का परिणाम है, नया ज्ञानोदय में छपी उनकी नई कहानी ‘यारेग़ार’... जिसकी आज मुक्त-कंठ से प्रशंसा हो रही है।
रचनाकार से इतर एक पाठक के रूप में उनकी यात्रा सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती गयी, जो आज भी उतने ही उत्साह से जारी है। एक पाठक से रचनाकार बनने के सफ़र में उनके क्या अनुभव रहे हैं… इस साक्षात्कार में पढ़िए।
नरेन्द्र कुमार : एक अच्छा लेखक होने के लिए जरूरी शर्त है अच्छा पाठक होना। आप किस हद तक इससे सहमत हैं?
दिव्या विजय : अच्छा लेखक होने के लिए अच्छा पाठक होना आवश्यक है। एक लेखक ही अगर किताबें नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन पढ़ेगा। नेपोलियन हिल के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जिसे वह पसंद ना करता हो।” यही बात लेखक पर लागू होती है।
यूँ तो पढ़ने के अपने फ़ायदे हैं। सभी लोगों को पढ़ने की आदत ज़रूर होनी चाहिए लेकिन दो लिहाज़ से लेखक के लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो उठता है। भाषा पर अधिकार के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भाषा की बारीकियाँ पढ़ कर ही सीखी जा सकती हैं। शब्दों को सही जगह पर बरतने की कला, निकट और दूरागत संदर्भ प्रयोग, वाक्यों का सही विन्यास, व्याकरण का शिष्टाचार, व्यंजना आदि भाषायी सोपानों के साथ प्रतीकात्मकता, भाव संप्रेषण की क्षमता भी नियमित पढ़ने से स्वयं भाषा में उतर आते हैं।
नये शब्दों को शब्दकोश से सीखने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, उस से अधिक नए शब्द, पढ़ने से अनायास ही पढ़ने वाले के शब्द-भंडार में एकत्रित हो जाते हैं। और फिर शब्द की सार्थकता उसके संदर्भ से होती है, कोशगत अर्थ बिना संदर्भ के अधूरा होता है।
पढ़ने से लेखक अच्छे और बुरे लेखन में फ़र्क़ करना सीख पाता है। कोई भी किताब क्यों अच्छी बनती है और क्यों बुरी, इसका रहस्य उसके भीतर के शब्दों में ही छिपा होता है। पढ़ते हुए एक लेखक का ध्यान उन बातों की ओर अवश्य ही जाता है/ जाना चाहिए। किताब का रुचिकर लगना, न लगना व्यक्तिगत रुचियों पर भी निर्भर करता है लेकिन फिर भी किताब के आकर्षक/अनाकर्षक लगने वाले अंश के प्रतिबिम्ब में अपने लेखन को परखा जा सकता है।
वे किताबें जिन्हें क्लासिक का दर्जा प्राप्त होता है उनमें एक यूनिवर्सल अपील होती है जो अधिकतर लोगों को आकर्षित करती है। सफल किताब के उस तत्व को रेखांकित करने का माध्यम पढ़ना ही बनता है। इस तरह पढ़ना लेखक के स्वयं के शिल्प को निखारने में मदद करता है। एक पाठक के तौर पर वह अपनी रुचियों को परखता है कि उसे कैसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है अथवा किसी किताब में उसे क्या बात सबसे अधिक पसंद आती है। उन्हीं बातों का समावेश वह अपने लेखन में कर सकता है। उसके अपने अनुभवों के साथ मिलकर नया सृजन भी होता है और परम्परित का संस्कार भी।
पढ़ते-पढ़ते कितनी ही बातें मन में आती हैं। उनमें से कितनी बातें लेखक की कृति का आधार बनती हैं। उदाहरण के तौर पर, पढ़ते हुए लेखक को कोई नया शब्द मिला और उस शब्द ने लेखक को इतना रिझा लिया कि वह अपने लेखन में उसका उपयोग अवश्य ही करेगा। किताब के किसी दृश्य से नया विचार उसके मन में उपजा तो एक नयी बात उसके लेखन में आप ही सम्मिलित होगी। यह बात एक शब्द अथवा विचार तक सीमित नहीं है। कभी-कभी पूरी कहानी या किताब तक के अंकुर ऐसे ही फूटते हैं।
हर व्यक्ति के जीवनानुभवों की एक सीमा होती है। जीवन की व्यस्तताएँ सबको एक-सा अवसर नहीं देतीं। सबके लिए अपने दायरे तोड़कर बाहर जाना सम्भव नहीं होता। ऐसे में किताबें उन स्थानों का, जहाँ जा पाना संभव नहीं, गवाक्ष बनती हैं। किताबें लिखने वाले के मन का वातायन भी होती हैं सो किसी के मन के भीतर झाँकने का अवसर किताबों से बेहतर कौन जुटा सकता है। मनुष्य के मन, मस्तिष्क के अध्ययन में अनुभव की सारथी भी बनती हैं किताबें। 'राइटर्स ब्लॉक' के धर दबोचने पर लेखक की नैया पढ़ने से भी पार लगती है।
अपनी बात कहूँ तो कितनी बार उदास दिनों और अकेलेपन की साथी किताबें ही बनी हैं। अपने एकांत से वार्तालाप को सघन करने का साधन भी हुई हैं किताबें।
नरेन्द्र कुमार : प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए आपको कब लगा कि पाठ्यपुस्तकें साहित्य के लिए कम पड़ रही हैं और आप साहित्य की अन्य पुस्तकों की तरफ गयीं। किस भाषा के साहित्य ने आपको शुरुआत में प्रभावित किया?
दिव्या विजय : पाठ्यपुस्तकों से साहित्य तक की ‘यात्रा’ अलग से कभी तय नहीं करनी पड़ी क्योंकि साहित्यिक पुस्तकें सदा जीवन में रहीं। मेरे नाना हिंदी के विद्वान रहे हैं। वह स्वयं भी कविताएँ लिखते थे। वह हिंदी के शिक्षक थे तथा उनकी लिखी पुस्तकें राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल थीं। उन पुस्तकों में नैतिक शिक्षा की कहानियाँ होती थीं जो सरल और बच्चों में पढ़ने के प्रति कौतूहल जगाने वाली थीं। अपने कोर्स के बाहर पढ़ने की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं पुस्तकों से हुई। एक ही शहर में होने के कारण मेरा बचपन का बहुत समय उनके साथ गुज़रा है और मेरे जीवन पर उन दिनों का गहरा असर है। जब मैं उनके यहाँ जाती उन्हें सदा पढ़ते-लिखते पाती थी। वह मुझे भी कोई किताब देकर बिठा देते। किताब मेरे लिए मिठाई सदृश थी। एक के ख़त्म होते ही दूसरी की लालसा जाग उठती। जल्द ही ऐसा समय आया जब उनकी किताबें चुकने लगीं और मेरी इच्छा बढ़ने लगी। तब मैं चोरी से वे किताबें पढ़ने लगी जिनके लिए मुझे लगता था वे मेरे लिए अर्थात बच्चों के लिए नहीं हैं। मामा और नाना से पूछे बिना उनकी किताबों की अलमारी से कोई पुस्तक निकालती और किसी कोने में, परदे के पीछे दुबक कर एक साँस में पढ़ जाती। एक बार मामा ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। तब मुझे काटो तो ख़ून नहीं। उन्होंने चुपचाप मेरे हाथ से किताब ली और किताब का नाम देख मुझे वापस पकड़ा दी। वह प्रेमचंद की कहानियों का संकलन था। किताब उन्होंने मुझे वापस दे दी थी लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि फिर से वह किताब पढ़ सकूँ। सारा दिन डर लगता रहा कि आज तो मामा, माँ से अवश्य शिकायत करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता, मेरे जाने के समय उन्होंने यह ज़रूर पूछा था कि किताब पूरी हो गयी या घर लेकर जानी है। और मैं जल्दी से ना में सिर हिला भाग खड़ी हुई कि किताब वाली बात माँ न सुन लें।
यही हाल मेरे घर में था। बच्चों की पत्रिकाएँ, ऊँट के मुँह में ज़ीरा सिद्ध होती थीं। एक सिटिंग में ख़त्म हो जातीं। फिर सिलसिला शुरू हुआ पढ़ने के लिए नयी किताबें ढूँढने का। चूँकि माँ भी हिंदी और संस्कृत की छात्रा, कालांतर में हिंदी की लेक्चरर रही हैं तो किताबों की कमी घर में कभी नहीं रही। इस सिलसिले में सबसे पहले हाथ आए कालिदास और जयशंकर प्रसाद के नाटक। आरम्भ में भाषा कुछ कठिन लगने पर भी धीरे-धीरे पढ़ना का प्रवाह बनता चला गया। बाद के दिनों में भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, अज्ञेय जैसे लेखक मेरे इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बन गए। माँ के कॉलेज की, उनकी लाइब्रेरी की जो किताब हाथ लगती वह पढ़ जाती। मेरे ज़िद करने पर पहले वह मेरे लिए बच्चों की कहानियाँ और नाटक लाती रहीं। उनके ख़त्म होने पर बाद में अच्छे लेखकों की किताबें छाँट-छाँट कर मेरे लिए लाने लगीं। मेरे स्कूल की लाइब्रेरी भी एक ज़रिया बनी। लेकिन हफ़्ते में एक किताब की सीमा बहुत खलती थी। रूसी कथा साहित्य से स्कूल की लाइब्रेरी गुलज़ार थी। सुंदर चित्रों वाली ये किताबें बार-बार मैं पढ़ती थी। इन्हीं दिनों शेक्सपियर को पहली बार पढ़ा और पढ़ती चली गयी। ऐसा नहीं था कि छुटपन में सब समझ ही आ रहा हो लेकिन निरंतर पढ़ते रहने से कुछ बातें सहज ही जीवन में समाहित होती चली गयीं। उनके लिए अलग से जतन नहीं करने पड़े। पापा मेरे लिए विज्ञान की किताबें लाते। मैं उन्हें भी समान रुचि से पढ़ जाती। बाद में यह आदत में शुमार हो गया। जो जहाँ मिले, पढ़ जाओ। इसी आदत ने चलते-फिरते बहुत कुछ पढ़वा दिया। हाँ, बाद के दिनों में मैं सिलेक्टिव हो गयी।
हिंदी और अंग्रेज़ी, दो भाषाएँ मैं जानती हूँ। इन दोनों भाषाओं में जो भी उपलब्ध होता, वह पढ़ती रही। किसी किताब को शुरू करने के बाद भाषा आड़े नहीं आती। लेकिन पढ़ने के लिए चुनाव करने की बात हो तो मैं पहले हिंदी की ही किताबें उठाती थी। आज भी यही करती हूँ।
नरेन्द्र कुमार : हिंदी साहित्य के अपने पाठन की शुरुआत से लेकर एक लेखक बनने तक आपको किन लेखकों ने अधिक प्रभावित किया? क्या यह पसंद भी समय के साथ-साथ परिवर्तनशील रही?
दिव्या विजय : बचपन में पढ़ने का शौक लेखक विशेष के नाम से प्रभावित हुए बिना पढ़ने और जो समझ आए उसके विरेचन भर तक ही सीमित था। जो समझ नहीं आता था उसे बड़ों से पूछने से हिचकती थी कि कहीं प्रश्न अवस्था का अतिक्रमण कर गया तो फिर किताब पढ़ने के सुख से भी वंचित न हो जाऊँ। हालाँकि झुकाव कथा साहित्य की ओर ही अधिक था। प्रेमचंद की कहानियों का गाँव या रेणु का गाँव, दोनों के आस्वाद की भिन्नता होते हुए भी दोनों ही समान रूप से आकर्षित करते थे। जैसा मैंने बताया कि बचपन में किताब मेरी लिए मिठाई सदृश थी, सो शुरूआत में पसंदीदा लेखक चीह्न कर पढ़ना शौक में अड़चन हो जाता।
बाद में जब मैंने निर्मल वर्मा को पढ़ा तब महसूस हुआ कि उनके वातावरण निर्माण में कमरे में मेज़ पर रखी रफ़ कॉपी से लेकर खिड़की से दिखती सड़क पर बस का इंतज़ार करते व्यक्ति तक को स्थान मिलता है। कहानी की मूल संवेदना का सूत्र पकड़े हुए पाठक को रोचक तथा नवीन शब्द प्रयोग मिलते हैं। वे कहते थे "ऐसा कई बार होता है कि घटना की स्मृति तो मिट जाती है बस उससे जुड़े शब्द रह जाते हैं। वे अलग हवा में झूलते हैं, मुझे ऐसे शब्द इकठ्ठा करने का शौक है।"
उनके पात्र अपने अंतर्द्वंद्वों से लड़ते हुए जब मौन रहते हैं तब उनके बीच के गैप्स को भरने के लिए बिजली के खंभे का आलोक वृत्त या नायिका की नाक की नोक पर थिर पानी की बूँद भी संकेत देती लगती है। वर्मा के साहित्य को पढ़ते हुए मन की उन अनखुली दराज़ों के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है जिनसे हम बेख़बर थे, जैसे रेडियो सिग्नल्स तो हमेशा हमारे बीच होते हैं पर वे हमें सुनाई तभी देते हैं जब हम रेडियो ऑन करें। दरअसल उनके लिखे में यथार्थ, स्मृति और कल्पना के बीच कहीं होता है जिसका सम्मोहन हमें खींचता है। एक ऐसा स्पेस जो अपरिचित होने पर भी हमारे अनुभूत यथार्थ को खण्डित नहीं करता। जहाँ ज़्यादातर लेखकों के लेखन को किसी वाद या वर्ग में बाँट दिया गया वहाँ वर्मा का साहित्य इनसे अछूता ही है।
पर अब तो विपुल साहित्य उँगलियों पर उपलब्ध होते हुए भी व्यस्त जीवन इतना अवकाश नहीं देता, तिस पर रुचि भी परिष्कृत हुई है। बचपन में सब कुछ पढ़ने का शौक अब सिलेक्टिव हो गया है। एक रचनाकार सामाजिक संदर्भों में अपने निजी अनुभव या अनुभूति को अपनी रचनाओं में प्रतिबिंबित करता है, कभी यही दृष्टि अब पठन के लिए चयनाधार बनती है, कभी क्लासिक उठा कर उसके क्लासिक होने के कारणों को जानने का कुतूहल भी तो कभी किसी किताब की माउथ पब्लिसिटी भी। बचपन में जितना समझ आता था उसके रस चर्वण के बरअक्स अब पठनानुभव के साथ आत्मलय और आत्मानुभूति भी विद्यमान रहती है।
नरेन्द्र कुमार : आप लेखक होने के साथ गंभीर पाठक हैं। क्या एक पाठक साहित्य पढ़ते समय संवेदना और वैचारिकी के अंतर्संबंध पर ध्यान दे पाता है या वह सीधे साहित्य के प्रवाह में बहता चला जाता है?
दिव्या विजय : इस बारे में पाठक से पहले मैं लेखक की बात करना चाहूँगी। क्या एक लेखक साहित्य सृजन में सम्वेदना और वैचारिकी के अंतर्संबंध को सायास आरोपित करता है? साहित्य वैचारिकी के लिए खूँटी की तरह व्यवहृत नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से दोनों के गुंफन में लेखक अनाग्रही भाव रखे। यदि आग्रह है तो फिर सम्वेदना सशर्त हो जाएगी और पाठक पढ़ते समय एक आरोपण महसूस करेगा। पाठक सचेष्ट ध्यान नहीं दे, यही उपादेय है। साहित्य में बहते समय सम्वेदना पाठक के मन पर रजिस्टर हो और वैचारिकी के प्रति एक रोमंथन उसके मन के तलघरे में ऐसे जमा हो जो किसी पक्ष-विपक्ष से मुक्त हो। वैचारिक रोमंथन की एक अलगनी मन में बँधे जहाँ पाठक रोज़मर्रा के कामों करते हुए भी अपने विचारों के गीले कपड़े लटकाए और सूखने पर उतारे तथा तहा कर रख ले। वृक्ष की फुनगी को यदि उच्चतम होना है तो जड़ों को गहनतम अँधकार चूमने पड़ते हैं। वैचारिकी को भी यदि गहरे जाना है तब उसे दबे पाँव जाना होगा, पाठक का ध्यान पढ़ते समय उस पर जाएगा तो वह अवरोध ही उत्पन्न करेगा। लेखक का स्वर स्व स्फुटन का हामी होगा तो पाठक संवेदना में श्लिष्ट वैचारिकी के प्रति स्वतंत्र हो व्यवहार करेगा। पृच्छित अंतर्संबंध के प्रति लेखक का आत्यंतिक आग्रह सम्वेदना को भी अति बौद्धिक बना देगा।
पाठक की पसंद को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं। कुछ पाठक विषय के उद्देश्य से, कुछ भाषा शैली के चमत्कार से, कुछ चरित्रों से भी प्रभावित होते हैं। वैचारिकी भी एक कारक हो सकता है लेकिन सम्वेदना उसकी वाहक होती है। कितनी बार हम कुछ पढ़ते हैं, प्रभावित होते हैं और दूसरों को उसे पढ़ने के लिए उकसाते हैं क्योंकि जो सुख हमें मिला वो बँटना चाहता है। दूसरे जब वही पढ़ते हैं तो हमेशा उसे पसंद नहीं कर पाते क्योंकि वही सहजानुभूति उन्हें नहीं हुई, उनका पूर्वज्ञान, अनुभव, संस्कार, आस पास का वातावरण सब उसमें बाधक बन गया। उनका मस्तिष्क एक ही वैचारिकी को अलग तरह से समझेगा और हमारा मस्तिष्क अलग।
नरेन्द्र कुमार : एक समय आता है जब पाठक को लगता है कि उसके मनोभावों की अभिव्यक्ति समकालीन साहित्य नहीं कर पा रहा है, तब वह साहित्य में अपना हस्तक्षेप दर्ज़ करता है। आपको कब ऐसा लगा कि हस्तक्षेप करने की जरूरत है?
दिव्या विजय : काल विशेष की वैयक्तिक और सामाजिक रुचि किसी काल को व्यष्टि प्रधान तो किसी को समष्टि प्रधान बनाती है, कभी पुराने मूल्यों के प्रति गहरी आस्था स्वीकृत होती है तो कभी इनके प्रति गहरी अनास्था और अस्वीकार का भाव विस्तार पा स्वतंत्र और मुक्त दृष्टि का विकास होता है। परन्तु हर प्रवृत्ति, हर मनोभावों की न्यूनाधिक उपस्थिति हर युग में होती है, बस कोई एक प्रधान हो जाती है। इसलिए हस्तक्षेप करने जैसा गुरूतर कार्य बतौर पाठक मुझे करने का भाव नहीं आया।
जो अनुभव सामान्य व्यक्ति को केवल एक भोक्ता बनाकर ही छोड़ जाते हैं, वहीं लेखन प्रतिभा और लेखन के प्रति औत्सुक्य से युक्त व्यक्ति को अद्भुत अनुभूतियों से गुज़ार कर भावसंपन्न बना जाते हैं। लेखक का मन किन्हीं अज्ञात और अनाख्येय कारणों से भावांदोलित होता है। स्वानुभूत मनोभावों का उत्प्रवाह, परानुभूत मनोभावों को सुन तथा ऑब्ज़र्व कर उनका स्मरण मात्र नहीं बल्कि एक मानसिक भावन की क्रिया मैं महसूस किया करती। मेरी सजग और संवेद्य कल्पना शक्ति सर्वांग भावन करके घटनाओं, पात्रों, मनोभावों आदि को मस्तिष्क में सजीव करने लगी। इन सबकी समवेत अंतः प्रेरणा ने मुझे अभिव्यक्ति मार्ग के अनुसंधान के लिए विवश किया और मैंने लेखन को अपनी अभिव्यक्ति के लिए चुना।
परिचय :
नाम - दिव्या विजय, जन्म - 20 नवम्बर, 1984, जन्म स्थान – अलवर, राजस्थान, शिक्षा - बायोटेक्नोलॉजी से स्नातक, सेल्स एंड मार्केटिंग में एम.बी.ए., ड्रामेटिक्स से स्नातकोत्तर
विधाएँ - कहानी, लेख, स्तंभ
‘अलगोज़े की धुन पर’ कहानियों की पहली किताब। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं जैसे नवभारत टाइम्स, कथादेश, इंद्रप्रस्थ भारती, पूर्वग्रह, जनपथ, नया ज्ञानोदय, परिकथा, सृजन सरोकार आदि में नियमित प्रकाशन। इंटरनेट पर हिन्दी की अग्रणी वेबसाइट्स पर अद्यतन विषयों पर लेख। रविवार डाइजेस्ट में नियमित स्तंभ।
अभिनय : अंधा युग, नटी बिनोदिनी, किंग लियर, सारी रात, वीकेंड आदि नाटकों में अभिनय। रेडियो नाटकों में स्वर अभिनय।
सम्मान - मैन्यूस्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट विनर, मुंबई लिट-ओ-फ़ैस्ट 2017
सम्प्रति - स्वंतत्र लेखन, वॉयस ओवर आर्टिस्ट
ईमेल- divya_vijay2011@yahoo.com