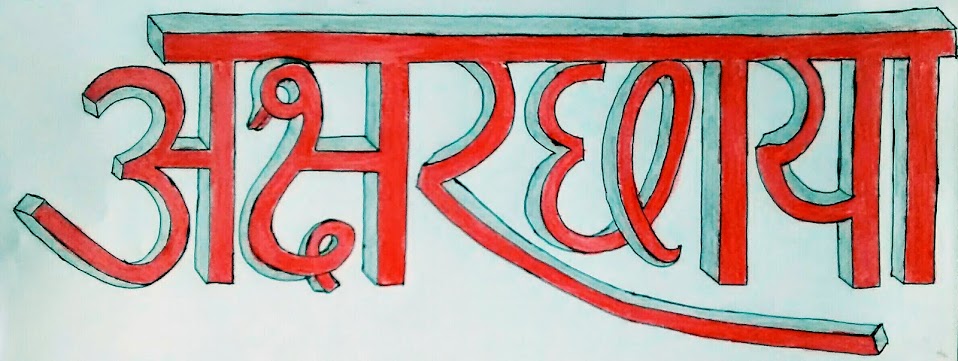22 जुलाई 2017 की सुबह...जे डी वीमेन्स कॉलेज, बेली रोड, पटना का ऑडिटोरियम आधी आबादी की सक्रिय मौजूदगी से जीवंत था। आखिर क्यों न हो, यह दिन 'आयाम–साहित्य का स्त्री स्वर' का स्थापना दिवस जो है तथा यह मौका उसके दूसरे वार्षिकोत्सव का था। 'आयाम' एवं जे डी वीमेन्स कॉलेज के साझे आयोजन का विषय था–समकालीन महिला लेखन : चुनौतियां एवं संभावनाएं। जाहिर है, चर्चा बिहार के विशेष संदर्भ में होनी थी।
तो इस आयोजन की शुरुआत हुई, मंगलाचरण से...सविता सिंह नेपाली की मधुर मखमली स्वर में सब खो ही तो गए थे। गीत था पंडित नरेन्द्र शर्मा का लिखा – 'ज्योति कलश छलके।' उसके पश्चात डॉ. मीरा कुमारी, प्राचार्या, जे डी वीमेन्स कॉलेज की अध्यक्षता में प्रथम सत्र की शुरुआत हुई...संचालन भावना शेखर कर रही थीं। सविता सिन्हा द्वारा 'आयाम' की स्थापना के उद्देश्य बताये गये। उन्होंने कहा कि विद्रोह का पहला क्षण अभिव्यक्ति है। दो साल पहले डॉ. उषाकिरण खान के निमंत्रण पर कई रचनाकार जुटीं तथा धूसर और लहूलुहान यथार्थ को अभिव्यक्त करने हेतु 22 जुलाई 2015 को 'आयाम' की स्थापना हुई।
इसके उपरांत डॉ. उषाकिरण खान द्वारा स्त्री-साहित्य पर बात रखी गयी। उन्होंने अफ़सोस जाहिर करते हुए कहा कि स्त्रियां घर से निकल बाहर तक तो आयीं हैं, पर उन्हें मान्यता नहीं मिली है। कोई भी पुरुष पहली कहानी अपनी दादी या नानी से ही सुनता है। बिहार के सौ साल के साहित्यिक इतिहास को ही देखा जाय तो महिला साहित्यकारों के कई उदाहरण मिलेंगे। रशीदन बी, बिन्दु सिन्हा, शांता सिन्हा आदि रचनाकारों की चर्चा कहाँ हो पाती हैं। हमारे साहित्यिक समाज में इनपर ध्यान देने की अहमियत नहीं समझी गयी। आज भी किसी महिला रचनाकार की कृति सराही जाती है या पुरस्कृत होती है तो यही बात उड़ायी जाती है कि किसी समर्थ या असमर्थ पुरूष अपनी रचना लिखकर उसे दे देता है। मैं कहना चाहती हूं कि फिर वे अपने लिए क्यों नहीं उस स्तर की रचनाएं लिख पाते हैं। आज महिलाएं संवाद करना चाहती हैं...विचार-विनिमय करना चाहती हैं। इस कारण ही 'आयाम' का आविर्भाव हुआ है।
अब बारी थी आलोचक डॉ. रोहिणी अग्रवाल की। उन्होंने कहा कि अपने सपनों का पीछा करते हुए पटना नहीं, पाटलिपुत्र आई हूँ। यहाँ आते ही दो साहित्यिक विभूतियां–रेणु और दिनकर याद आते हैं। रेणु के 'मैला आँचल' की कई पात्रों से होते हुए दृष्टि मठ के महंत के शोषण तले छटपटाती लक्ष्मी पर जाती है। बिहार और उसके बाहर आज भी कई लक्ष्मी अपने वजूद के लिए संघर्षरत है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि लक्ष्मी का शोषण महंत नहीं, बल्कि धर्म की सत्ता कर रही है। यह सत्ता मनुष्यता को खंडित करती है। धर्म सांस्कृतिक प्रवंचनाओं का मोहक रूप लेकर सामने आता है। आज के स्त्री-लेखन की असल चुनौती इन्हीं प्रवंचनाओं से है जो संस्कृति को स्त्रीत्व का पर्याय बताती हैं।
रोहिणी अग्रवाल ने आगे कहा कि दिनकर की 'उर्वशी' में दृष्टि उर्वशी और पुरुरवा के मांसल प्रेम से इतर सुकन्या पर जाती है। वह कहती है कि जिसने हमें सिरजा था, वह प्रकांड पुरूष था, इस कारण उसने पुरुष को स्वत्त्व हरण की प्रवृत्ति दी तो स्त्रियों को अपने अधिकार गँवा कर कृतार्थ होने की। सुकन्या आगे कहती है कि अगर उन्हें सृजन का निर्बाध सुयोग मिला तो ऐसे पुरुष की रचना करेंगी जो उनकी मौन-व्यथा को सीधे सुन सकेगा। इस तरह दिनकर स्त्री-संवेदी पुरुष की कल्पना करते हैं।
अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि 'कठगुलाब' में मृदुला गर्ग एवं 'डाउनलोड होते हैं सपने' में गीताश्री स्त्री-संवेदी मन की गहराई में जाती हैं। अपने सपनों को पीछा करने की दृढ़ता एवं आकाश खोजने की जिद ही तो संभावना है। कमलेश्वर की कहानी 'तलाश' में विधवा मां अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, पर यहां बेटी ही विरोध कर देती है। वहीं कविता की कहानी 'उलटबांसी' में सत्तर साल की मां का साथ उसकी बेटी एवं पोती देती है।
उन्होंने आगे कहा कि पुरूष लेखन अपने अंदर नहीं झाँकता, जबकि स्त्री अपने भीतर अपने आपको ही मथती है यानी स्त्री लेखन आत्मालोचना है। आज की स्त्री को पितृसत्ता की सही समझ है। वह धर्म एवं संस्कृति द्वारा रची गयी प्रवंचनाओं का विरोध करना जानती है। वह जानती है कि स्त्री देह नहीं विवेक है। धार्मिक संस्कार स्त्रियों को याचक बनाते हैं। आज की महिला रचनाकार धर्म के सही स्वरूप को पहचानती है। मधु कांकरिया अपनी रचना 'सेज पर संस्कृत' में बताती हैं कि धर्म विवेक को कुंद करता है। स्त्री के भीतर का हाहाकार पितृसत्ता के खिलाफ है और इसका शिकार स्वयं पुरुष भी है।
साहित्य और यथार्थ के संबंध पर उनका कहना था कि "साहित्य यथार्थ का ज़ेरॉक्स नहीं है। आम आदमी जो नहीं देखता, उसे साहित्यकार देखता है। वह इहलोक के समानांतर एक लोकोत्तर सत्ता है।" स्त्री रचनाकारों के बोल्ड लेखन पर उनका कहना था कि पुरुष बन जाना स्त्री-लेखन का अभीष्ट नहीं है। यह तो देह एवं दैहिक संबंधों को चिकन या रसगुल्ला की तरह पेश करना हुआ। कवयित्रियों के संबंध में उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं की गयी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे कविताएं अधिक नहीं पढ़ पातीं।
डॉ. रोहिणी अग्रवाल के वक्तव्य के पश्चात डॉ. मीरा कुमारी, प्राचार्या, जे डी वीमेन्स कॉलेज के अध्यक्षीय भाषण से इस सत्र का समापन हुआ। इसके बाद नीलाक्षी सिंह द्वारा उनके आनेवाले उपन्यास-अंश का पाठ किया गया। फिर अलका सरावगी द्वारा उनके प्रकाशनाधीन उपन्यास 'एक सच्ची-झूठी गाथा' के अंश का पाठ किया गया। दोनों लेखिकाओं का कथा-पाठ बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा।
भोजनावकाश के पश्चात वरिष्ठ आलोचक खगेन्द्र ठाकुर की अध्यक्षता में कविता-सत्र आरंभ हुआ। सत्र का संचालन रानी श्रीवास्तव कर रही थीं। संध्या सिंह, मीरा श्रीवास्तव, अंजना वर्मा, पूनम सिंह, रश्मि रेखा, प्रतिभा चौहान, भावना एवं पंखुरी सिन्हा द्वारा प्रवाहमय काव्य-पाठ सुनने का अवसर श्रोताओं को मिला। उनमें आधी आबादी के सपने भी थे तो संघर्ष भी...लोक का आकर्षण उनकी कविताओं में था तो सुदृढ़ परंपरा के प्रति आदरभाव भी। आयोजन में हृषिकेश शुलभ, कर्मेन्दु शिशिर, शिवदयाल, शिवनारायण, अवधेश प्रीत, निवेदिता झा, सुनीता गुप्ता, नताशा, अरुण नारायण, सुशील कुमार भारद्वाज, बालमुकुन्द, सत्यम कुमार, नरेन्द्र कुमार आदि रचनाकारों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही
अंत में सुमन सिन्हा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन हुआ और 'आयाम' का दूसरा वार्षिकोत्सव अपनी पूरी सार्थकता के साथ संपन्न हुआ।