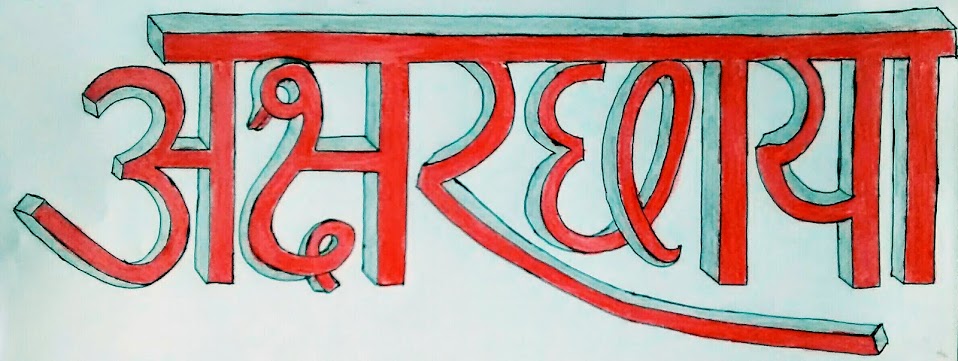एक सामान्य पाठक कविता में क्या चाहता है ? ...कि उसमें उसके वातावरण की निर्मिति हो, समय के साथ उत्पन्न होते उसके सुख-दुःख अभिव्यक्त हों तथा उसके प्रश्न उनमें शामिल हों। गौरव पाण्डेय की कविताओं से गुजरते समय वह ऐसा ही महसूसता है ...उससे जुड़ने लगता है और यहीं पर उनकी रचना सार्थकता को प्राप्त होती है।
" समकालीन हिंदी कविता की लोकचेतना " विषय पर शोध करनेवाले कवि की रचनाओं में उनकी जमीन, भाषा एवं लोक अनायास ही आते हैं तथा कविता अपनी रौ में आगे बढ़ जाती है। उनकी रचनाओं में संबंधों की गहराई का सूक्ष्म चित्रण है तो गांव-जवार से पलायन करते मजबूर लोगों का दर्द भी।
अक्सर हम कई कविताओं को पढ़ने के क्रम में पाते हैं कि बिंब सहजता से नहीं बन रहे हैं और कवि इधर-उधर के संपर्क-सूत्रों का बेवजह इस्तेमाल करने लगता है। इससे कविता का प्रवाह टूटने लगता है तथा भाव एवं सौंदर्य भी प्रभावित हुए बिन नहीं रह पाते। पर गौरव पाण्डेय की कविताओं में बिंब स्पष्ट बनते हैं...प्रवाह और सौन्दर्य तो लाज़वाब ! उनकी कविताओं का शिल्प अलहदा है तथा संवाद का बेहतरीन प्रयोग देखने लायक है। तो आइए, देखते हैं।
1. गांव से निकले बहुत लोग
गांव से निकले बहुत लोग
कुछ न कुछ करने
और लौटे भी
जो कुछ बन पड़ा वो करके
लौटे कुछ ईंटा-गारा करके
बोझा ढोकर लौटे कुछ
देर शाम तक
नमक-तेल-तरकारी लिए बहुत लौटे
कुछ ऐसे थे
जो लौटे बहुत दिनों बाद
बड़ा-सा बैग, रुपया, कपड़ा और सपने लेकर
लेकिन कुछ ऐसे भी थे
जो नहीं लौटे
खो गए
जो नहीं लौटे
उनमें अधिकतर ऐसे थे
जो कुछ हो गए
वे डॉक्टर, वे प्रोफेसर, वे वकील
वे पत्रकार, वे थानेदार
ये जहाँ गये वहीं के रह गये थे
इधर जिनके लौटने की उम्मीद
खो चुका था गांव
वे मृतकों के बीच से उठकर लौटे...
●●
ये नायक
गाँव के बेटे थे
अब दामाद की तरह लौटते थे
गांव बीमार था
डॉक्टर इलाज करने नहीं आया
और निरक्षर गांव ने
प्रोफेसर से एक अक्षर नहीं पाया
वकील ने गांव को नहीं दिया कोई न्याय
और पत्रकार क्या जाने गांव का हाल-चाल
दरोगा ने रौब दिखाया गांव को ही
जब कभी
दिया गया इन्हें कोई सम्मान
तब जरूर चर्चा में रहा गांव का नाम... ...
2. मजदूर औरतें लौट जाती हैं
मजदूर औरतें
आती हैं दूर-सुदूर के गांवों से
दिन-दिन भर खेतों में काम करती हैं
रोपती हैं धान, खर-पतवार साफ़ करती हैं
अकेली नहीं आतीं ये
बहू, बेटी और पोतियां साथ लाती हैं
साथ होती हैं पड़ोस की तमाम मजदूर औरतें
पानी से भरे लबालब खेत में
सकेल कर साड़ी, कमर में बांधकर दुपट्टा
मारकर कछोटा छप्प्-छप्प कूद जाती हैं
एक-दुसरे पर फेकती हैं गीली मिट्टी-कीचड़
अंजुरी भर-भर छींटे मारती हैं
समवेत स्वर में हँसती हैं
ये अलग-अलग उम्र की औरतें
मिट्टी-पानी के मिलन रंग में रंग जाती हैं
दादी-चाची-माँ-बेटी-नन्द-भउजाई
जब खेत में ही होने लगती है झमा-झम बारिस
बच्चियों संग बच्चियां बन लोटती-पोटती हैं
शगुन मनाते रोपनी के गीत गाती हैं
इस तरह कब रोप देती हैं ये दस-दस बीघे धान
हँसते-खेलते-उछलते-कूदते-गीत गाते
पता ही नहीं चलता
पता ही नहीं चलता दिन के अंत का
और ये अपनी हंसी-किलकारी खेतों में छोड़कर
रोपी गयी फसलों के प्रति निःस्पृह होकर
लौटने लगती हैं
कुछ रुपया मुट्ठी में दबाये, आँचर में गठियाये
कल कहीं और रोपनी की बात करते हुए
लौट जाती हैं
ये मजदूर औरतें
3. मजूरिनों के बच्चों का खेल
शिक्षकीय भवन का कार्य
प्रगति पर है
तोड़ रही गिट्टियां औरतें
कुछ ढो रही ईंट, चाल रहीं बालू
नंग-धड़ंग बच्चे खेल रहे आस-पास
यह जुलाई की दोपहर है
कुछ बच्चे आते दौड़े-दौड़े
पास से गुजरने वालों के
पैरों के बहुत पास
लोट जाते
लोग पीछे हटते
बच्चे धूल झाड़ते उठते
मुस्कुराते...ये खेल था उनका।
खेल रहे कुछ और बच्चे
मिट्टी से नहीं ईंट के टुकड़ों से..
उछालते हैं तपते सूरज की ओर
साधते है निशाना बादल के टुकड़ों पर
फेंकते हैं क्षितिज की ओर
हम भी पुस्तक लिए गुजरते हैं
वे देखते हैं हमारी तरफ
हवा में उछालते हैं
ईंट के टुकड़े
हम डर जाते हैं
वे सब साथ मुस्कुराते हैं
चिढ़ाते हैं
ईंट के टुकड़े हाथ में ही दिखाते हैं
इस खेल में
हम ग्लानि से भर जाते हैं
कुछ सोचकर क्षण भर को ठिठकते हैं
फिर उन्हें पीछे छोड़
पुस्तक कांख में दबाए आगे बढ़ जाते हैं।
4. माँ गौरैया होती है
माँ भोर में उठती है
कि माँ के उठने से भोर होती है
ये हम कभी नहीं जान पाये
बरामदे के घोसले मे
बच्चों संग चहचहाती गौरैया
माँ को जगाती होगी
या कि माँ की जगने की आहट से
शायद भोर का संकेत देती हो गौरैया
हम लगातार सोते हैं
माँ के हिस्से की आधी नींद
माँ लगातार जागती है
हमारे हिस्से की आधी रात
हमारे उठने से पहले
बर्तन धुल गये होते हैं
आँगन बुहारा जा चुका होता है
गाय चारा खा रही होती है
गौरैया के बच्चे चोंच खोले चिल्ला रहे होते हैं
और माँ चूल्हा फूंक रही होती है
जब हम खोलते हैं अपनी पलकें
माँ का चेहरा हमारे सामने होता है
कि माँ सुबह का सूरज होती है
चोंच में दाना लिए गौरैया होती है ।
5. कंचे खेलती पत्नी
यह ठिठुरती शाम है जनवरी की
द्वार पर पडोसी-बच्चे
खेल रहे कंचे
शोर करते
हम सब चाय पी रहे... ...
चाय पीते न्यूज़ देख रहे पिता, भाई मोबाईल में कुछ
पत्नी और बहन देख रहीं कंचे खेलते बच्चों को
बरामदे में बैठा थाम रहा मैं किसी नाजुक
कविता का हाथ
अचानक आवाज आई हँसती हुई माँ की
"अरे...अरे देखो दुआरे देखो
दुलहिन गोली खेल रही गदेलन के साथ..."
उनकी हंसी में इक ख़ुशी थी
लेकिन मना कर देने का आग्रह भी अगले स्वर में
"अबहिन कोऊ देखी तौ का सोची बेटवा, नई दुलहिन......"
मैंने देखा वह खेल रही
छोटे-बच्चों के बीच कोई बच्ची सी
एक हाथ संभाले आँचर का छोर
फिसल न जाये माथे से
साध रही निशाना दूसरे हाथ से
बहन हँस रही, पास खड़ी "भाभी ऐसे नहीं ऐसे, इधर लगाओ निशाना .....उधर नहीं"
मैंने भीतर देखा टीवी देख रहे पिता चुप थे
भाई की नजरे टिकी थी मुझ पर कि शायद मैं कुछ कहूँ
हंसी के बीच मना कर देने का एक भाव था चेहरे पर माँ के
मैं देखता रहा इस कौतुहल बीच
वह चल रही चाल अपनी
साध रही निशाना
निशाना गलत लगे
बच्चे मन में यही सोचते
रोमांच से भरे
अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते
मैंने चिल्ला कर कहा- "ओये~~~"
उसने मुड़ते हुए कहा- " क्य्य्या~~~"
क्या के साथ चली आई एक हंसी कंचों की खनक सी
मैं मुस्कुरा उठा "नहीं... कुछ नहीं "
खेल कर लौटी कुछ देर में
आते ही पूछ बैठी,- "चिल्ला क्यों रहे थे ?"
मैंने कहा-"बेइज्जती कराओगी क्या मेरी ?
आ गयी हार कर, मैं कभी नहीं हारा कंचों के खेल में"
उल्लास में कहा उसने-"ओये हेल्लो...
क्या समझते हैं, जीत के आये हैं... देखिए जरा उधर..."
साथ देखा सबने
बच्चे खड़े थे हारे हुए
इधर ही देखते सारे खिल-खिल हँसते हुए... ...
6. पत्नी : बहन और माँ
कभी-कभी
पत्नी को देखता हूँ
जैसे देखता हूँ बहन को
चाहता हूँ लगा दूँ एक आलपिन
फिसलते दुपट्टे पर
कालेज-बैग तैयार कर छोड़ आऊँ चौराहे से पार...
कभी-कभी
उससे लिपटते हुये
भर जाता हूँ एहसास तक
और उसके सीने में दुबके हुये
याद आ जाती है माँ...
कभी-कभी
वह बेतहाशा चूमती है
फेरती है हाथ
जैसे मैं अभी-अभी किसी हादसे से बचकर आया होऊँ.....
कभी-कभी
जब वह सो रही होती है मेरे बगल में
तब निहारता हूँ उसके चेहरे को
निहारता हूँ जैसे माँ को या सोयी हो जैसे छोटी बहन...
7. धत्त ऐसे भी कोई देखता है क्या ?
चाय की एक हल्की चुस्की लेते हुए
मैंने उसे ऐसे ही देखा
गर्दन टेढ़ी किये
बालों से पानी झाड़ते उसने मुझे देखते हुए देखा
मैंने फिर देखा
उसने फिर मुझे देखते हुए देखा
मैंने नजर फेरते उसे बालों से उलझते हुए देखा
तनिक खीझते देखा
गहरी चुस्की के साथ कप नीचे रखते हुए
उसे चोर नजरों से देखने के लिए मैंने सोचते हुए देखा
चोरी पकड़ जाने के डर से मुझे असहज होते हुए
उसने देखा
वह मुस्कुरा उठी, फिर उसने मुस्कुराते हुए देखा
बालों को मुठ्ठी में पकड़ गोल लपेटते हुए उसने
चिढ़ती आँखों से देखा- "क्य्य्य्या !"
कुर्सी पे पीठ टिकाते, सिर न में हिलाते ,आँखों की
भरपूर गहराई से
जवाब देते - " नहीं... कुछ तो ..नहीं" मैंने देखा
एक मुस्कराहट के बीच हमारी पलकें झुकीं
हम हँस पड़े
हम एक साथ हँस पड़े.... हँसते रहे
साड़ी के पल्लू पर पिन लगाते, अपनी हँसी को सयास रोकते
उसने कहा-
"धत्त ...अब ऐसे भी कोई देखता है क्या !!"
इस पर
अर्थ भरी मुस्कान लिए
हमने एक- दूसरे को फिर देखा.... ।
8. तुम्हारा एक भाई सुन रहा है
दादी के पास
कई लंबी कहानियाँ थीं
परिवार के साथ पडोसी भी सुनते थे
लेकिन दादी के पास एक और कहानी थी
जिसे किसी ने नहीं सुना कोई नहीं जानता उसे
माँ को कहानी कहने की फुरसत न थी
उसने कहानी नहीं कही
हमसे भी
बस एक अस्पष्ट-सा गीत गाती रही मॉ
जिसे आँगन में खेलते कभी-कभी हम सुनते रहे
आओ !
दादी की उस कहानी को लिखें
माँ के अबूझ गीतों को सप्तम सुरों में गाएँ...
मेरी बहनो !
तुम चुप मत रहो मन की कहो
आओ गाओ-गुनगुनाओ प्रतिरोध रचो.....
देखो !
पूरा विश्व सुन रहा है......
और घर में
कोई सुनें न सुनें
तुम्हारा एक भाई सुन रहा है......
9. कजरी : गँवई प्रेम-कथा
सूरज के उठने से बहुत पहले
वो उठती
साथ उठती उसकी पायल
उधर खेतों में अलसाई फसलें उठतीं
फसलें बजती
इधर कमर में घुंघरू
घुंघरुओं का शौक देखिए
बकरियों के पैरों में उसने बांध रखे थे कुछ घुंघरू
छुन-छुन-छुनुन-छुनुन-छुन-छुन्छुन
उधर से कोई गुजरता
झाड़ू लगाते
कभी लोटा लिए खेतों की ओर जाते
नहीं तो कुछ देर बाद बर्तन मांजते या कुँआ के पास
रस्सी-बाल्टी लिए दिख ही जाती
दोपहर दो के बाद
खेतों की ओर बकरियों का झुण्ड लेकर जाते
उसे प्रायः देखा जा सकता था
बकरियों के पीछे दौड़ते-भागते ही तो उसकी शाम होती
घुंघरुओं से गूंजते रहते खेत-खलिहान
ऊसर-बंजर नदी-नहर
जब बाप गुजरा और माँ उसके चाचा के साथ बैठी
वह बहुत छोटी थी
चाचा के चार बच्चों का गूं-मूत करते बड़ी हुई
नाम कजरी
लेकिन गेंहुआ है उसका रंग
गेहुअन सांप सी लोटती है सबकी छाती पर
रात-रात भर सपनों में बजते हैं घुँघरू
कुछ बौराये गली-गली यही कहते-फिरते
अच्छे भले स्वाभाव के लड़के उधर ठहर जाते
पचास पार के कुछ पहुँचे हुए
लफंगों को कोसते गरियाते खुद को छिपाते बातें-बनाते
कितनी इच्छा थी
कि एक बार वे बकरी के बच्चे हो जाएँ
उन्हें वो प्यार से सहलाए
इतना ही नहीं वे यहाँ तक चाहते थे
अगर वो प्यार से बाँध दे दो घुंघरू
तो बकरियों के साथ वह भी घास चर आएं
नांच-नांच जाएँ
छुनुन-छुनुन
अरहर के खेतों ने कजरी को बार-बार आमंत्रित किया
बाजरा और जोन्हरी ने झुक-झुक छुआ
सांझ के धुंधलके ने हाँथ पकड़ा
आने-जाने वाले टकराते रहे
पगडंडियों में बार-बार
लगातार
कजरी
किससे क्या कहती ?
जब तक हो सका अपने रास्ते आती जाती रही
छुन्न~~~छुन्न~~~~छुन
धीरे- धीरे बंद हुआ उसका बकरी चराना
फिर खेतों की ओर अकेले जाना
फिर कम दिखी कुँआ से पानी भरते
फिर द्वार के दरवाजे पे दिखती रही कभी-कभी
छुन्न-छुन
आखरी बार उसे कब और कहाँ देखा गया
नहीं पता
किसी को नहीं पता
कई कहानियां हैं
लोगों की तमाम बातें हैं
एक कहानी
गाँव के परधान और कजरी के घर वालों के पास है
पड़ोसियों के पास है एक अलग कहानी
एक कहानी कजरी की सहेली के पास है
एक कहानी बकरियों के पास है
एक-एक खेतों-खलिहानों, पेड़-पौधों
और तालाब के पास है
घर के दरवाजे और कुँए के पास है
चारपाई और चूल्हे के पास है
मेरे पास कजरी की दो कहानियां हैं
अव्वल वह जिसे कजरी की सहेली ने अपने प्रेमी को बताई (जो कवि का मित्र है)
कहना है कजरी ने उसे कसम देकर सुनाई कि वह किसी से न बताये
दूसरी कहानी वह है
जिसे कजरी के बहुत दिनों तक गायब होने पर तालाब ने बकरी के बच्चे को सुनाई
उस बच्चे की दोस्ती एक छोटी बच्ची से थी
जो अभी बोलना सीख रही थी
उसने टुकड़ो में ये कहानी उसे सुनाई जिसे उधर से गुजरते बादलों ने सुन लिया
वही कहानी अँधेरी रातों में कभी-कभी बरसती रही
आज उसे ही बूंदों की लिपि में भीगते हुए कवि चुपचाप सुन रहा है
छुनुन-छुनुन-छुन-छुन्छुन
10. प्रेम में डूबे कवि का मृत्यु-संवाद
मृत्यु..!
तुम्हें नहीं जानता
ठीक ऐसे ही नहीं जानता था उसे
फिर भी
एक दिन वो आई
हज़ार-हज़ार कल्पनाओं के बीच से
अलग-थलग रूप धरती
इस मोड़ से उस मोड़ तक साथ चलने की
तमाम संभावनाएं लिए
उसने अपने होंठ रखे मेरे माथे पर
छाती पर रखा अपना सर
वर्षों के उद्यम से संचित हर कुछ
छोड़ कर
उसकी गोद में ली एक झपकी
स्वप्न में बहुत देर तक महकता रहा एक फूल
उसने मुझे बताया
दूब की नोक पर ठहरी ओस-बूँद है हमारा जीवन
फिर प्रेम क्या है ?
प्रेम....!
उस बूँद के भीतर तिरती (उलझी) नन्ही किरण..!
तितली
फूलों के रंग
चिड़ियों का शोर
झरनों की कल-कल
और होंठों पर चुम्बनों के निशान
क्या एक दिन सब मिट जायेंगें ! खत्म हो जाएंगे..!!
मृत्यु !
प्रियवयस्य..!!
हजार न-नुकुर के बावजूद
तय है तुम्हारा आना
और तय है तुम्हारे आने का वह दिन
सोचता हूँ क्या तुम्हारे आने से खत्म हो जायेगा सब कुछ
जैसे उसके चले जाने से !
●●
ओ अतिथि !
बरामदे में तुम्हारा स्वागत है
बैठो
प्रतीक्षा करो मेरे भीतर की कविताओं के
चुक जाने की
साँस में
घुली किरण के बुझ जाने की
प्रतीक्षा करो ।
●●
दुःख में होता हूँ दुखी
रो लेता हूँ
कह देता हूँ नाराजगी
सह लेता हूँ
देखता हूँ
बची हुई उम्मीद को घेर रखा है
लाख नाउम्मीदियों ने
फिर भी नहीं होता हूँ उदास
उदास हो भी जाऊं
जीवन में,
लेकिन नहीं चाहता उदास हों मेरी कविताएं
नहीं चाहता लिखना उदास कविताएं
इसलिए
मृत्यु-संवाद
और इस कविता की हर बात
यहीं चुपचाप स्थगित करता हूँ .....
आगे बढ़ता हूँ।
संपर्क :
गौरव पाण्डेय
शोध छात्र, हिंदी विभाग
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
मोबाइल - 09125099299