संजय कुमार शांडिल्य कहते हैं―"कथाओं में प्रायः विजय के आख्यान रहते हैं, कविता पराजय का संबल होती है। इन्हें पढ़–सुनकर मनुष्य हार कर भी जीवित रह सकता है।" हम उनकी कविताओं में यह स्थापना बनते देख सकते हैं। वे निजी एवं स्थानीय समस्याओं एवं परिस्थितियों को अन्य पक्षों के साथ जोड़कर देखते हैं। ये पक्ष विस्थापन, टूटते-छूटते परिवार, महत्वाकांक्षा के पीछे भागते इंसान और उससे उत्पन्न एकाकीपन आदि से जोड़कर बनते हैं। वे दुनिया को बेहतर देखना चाहते हैं। एक शिक्षक होने के नाते उनका दायित्व और बढ़ जाता है। रचनाओं में भी यह दायित्व बखूबी नजर आता है। उनका पहला काव्य–संग्रह 'आवाज भी देह है' बोधि प्रकाशन से छपकर पाठकों के बीच आ चुका है। अतः अधिक कहने से बेहतर है कि उन्हें कविताओं के माध्यम से जाना जाय।
तुम हमारी आवाजें खा रहे हो
रूई के फाहों सी
हवाओं के दस्तक सी
निरपराध आवाजें।
यह शोर, इसकी आँखें हैं
जिस पर काली पट्टी बँधी है
मस्तिष्क है जिसमें उन्माद भरा है
इसके हाथ हैं लोहे के।
समुद्र के खारेपन से भरा
इस शोर में इस शोर की
जकङी हुई देह है
कभी-कभी आ सकता है तरस
पराजय का परचम है
शिकारी के पिंजरे
सहानुभूति फँसाने के लिए।
पृथ्वी की सारी कविताएँ
सदियों के साझेपन के गीत
हमारे संग-साथ के अनुभव
इन्हें उत्तेजित करता है
आदमखोर होने के लिए।
यह शोर नरभक्षी है
हमारी आवाज़ खाने आया है
हमारी आवाज जैसे
पहाड़ पर पानी की लकीरें।
पानी की लकीरें
उपत्यकाओं से मैदानों तक
मैदानों से खेतों में
खेतों से घरों तक
यह शोर नरभक्षी है
नदियों और तालाबों को
देहों की नीली जलकुम्भियों से
भरती इसकी क्रूरता।
हम बचाएँगे पानी की लकीरें
यही धान की बालियाँ होंगी
इन्हीं से गेहूँ के कल्ले फूटेंगे।
सिर्फ आँत, जिगर और दिल ही नहीं
आवाज़ भी देह है मनुष्य की।
2. पृथ्वी के छोर
यह पृथ्वी का एक छोर है :
गाँव पहाड़ की तलहटी है
जहाँ एन्डीज़ मिल रहा है
सपाट मैदानों से
पेरू की किसी लोक भाषा में
कचरा बटोरने का गीत है
घोङे की बग्घी में
पुरूष जब विलासिता के
कार्टुन चुनने निकलेगें
हाथों को काम करता देख
होंठ उन्हें अपने आप गाएंगे।
स्त्रियाँ पास ही शहरी इलाकों में
बच्चे सँभालने निकलेगी
बच्चे ईश्वर सँभालता है
उसी लोक भाषा में यह भी
एक गीत है पृथ्वी के उसी छोर पर।
यह पृथ्वी का दूसरा छोर है
मेरे पङोस में :
मूँज के पौधों में सिरकंडे होने से पहले
सपाट मैदानों के भी अपने पहाड़ हैं
जिनकी तलहटियों से
कुछ स्त्रियाँ खर निकालने निकलेगी
कुछ रह जाएंगी गोबर पाथने।
अभी सरोद की तरह बजेगी पृथ्वी
मूँज धूप में सूखेगा
झूमर और कजरी के गीत साथ-साथ
झरेंगे
लकङियाँ और पत्ते पास के
जंगल से इकट्ठा कर
पुरूष घर लौटेगा।
यहाँ की लोक भाषा में भात
बनने का भी एक लोकगीत है।
फिर किसी सस्ती सी आँच पर
प्रेम वहाँ भी पकेगा और यहाँ भी
एक साथ रात की देह गिरेगी
ओस की तरह
श्रम से दुनिया को भरती हुईं
सुबहें ऊगेंगी
खाली जगहों में
लकीरों की तरह
हम दुनिया के छोर पर
काम करते हुए लोग
सुबह की इन लकीरों को
कविताओं में पढेंगे।
3. प्रवासियों का गीत
उन फर्शों को जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाया
हम उनपर बिना अपने पैरों के निशान छोङे चलते हैं
और हम ऐसे रहते हैं जैसे चील की चोंच में मांस के लोथड़े
टेम्स के मुहानों पर ,अरब सागर की उठी हुई चौपाटियों में ।
हमारे नाम उनकी भाषाओं में भद्दी गालियाँ हैं
शब्द कोशों में जगह बनाते
और स्थानीयता की हिंसा में मारे गए अजनबियों में
हमारी पहचान हमारी सोखी हुई शक्लें हैं
कोसी और नील के बासिन्दे हम
कोसी और नील की विपदाओं से बने हुए ।
बाँस की फट्टियों की तरह गंदे सीवर में उतरते हमारे पाँव
फैक्ट्रियों में मशीन की तरह इस्तेमाल होते हमारे हाथ
जूट और कपास जैसे हाथ, हिरणों और बारहसिंघे जैसे पाँव
वे पाँव जिनकी छापे हैं सहरसा और मेन्या की गलियों में ।
हमारा शहर इसी पृथ्वी पर
हमारे गाँव इसी धरती के
इब्न कासिब की महबूबा
रेणु का मैला-आँचल ।
नील और कोसी के किनारोँ से उतरे हम
अरब और उत्तर सागर तक
हमारे पसीने की इमारतें हैं, सङक है, फ्लाई ओवर है
ट्यूब और मेट्रो ट्रेन है, मुम्बई का लोकल भी ।
अपराधियों की सूची में शामिल हम जिन थानों में उनकी जनसंख्या में नहीं हैं ।
वर्तमान जब हमारा मजाक बनाता हमसे हमारा
वजूद पूछता है
रात की भीड़ के अकेलेपन में हमारी आत्मा से
इतिहास झङता है:
हम जहाँ के फराओ खुफु जहाँ के मंडन मिश्र ।
हमारी मिहनत से लंदन है ,हमारी मिहनत से मुम्बई
इब्न बतूता और मेगास्थनीज से पूछना-
वे जगहें जहाँ से हम आए और बदल गए पुतलों में
वे जगहें मिश्र और भारत की दुल्हनें हैं ।
बारिश थोड़ी कम होती, बाढ़ थोड़ा अधिक आता
अपनी माटी की उर्वरता और कपास और जूट के हम
बादलों से अधिक सघन, हवाओं से नर्म
रेशम से अधिक मूलायम और मजबूत
सिर्फ जगहें ही नहीं शक्लें भी विस्थापित होती हैं
इन्हें हमारी पेशियों का दर्द खींचता है ।
4. चाँडाल
परिदृश्य की हर मृत्यु
हमें एक भावी मृत्यु के लिए
तैयार करती है
वह चाँडाल जो दाह से पूर्व
स्वाँग करता है रूठने का
सिर्फ वही जीवन की तरफ से
व्यवधान पैदा करता है
धू-धू कर ध्वंस हो रहा है
कहीं निर्माण की नगरी से
विमुख न हो उठे यात्री
भवन से भुवन तक
सब माँगता है चाँडाल
फिर एक सौ एक, इक्यावन अथवा
ग्यारह पर राजी हो जाता है
हम जो मोलभाव करते हैं वहाँ
जहाँ सबकुछ एक आहुति है
वह उस चाँडाल का अनंत काल
से निर्मित स्वांग है
अगली मृत्यु तक वह हमें
पीछे हमारी दुनिया में
धकेल रहा है
निस्पृह जलती हुई चिता से
अपनी कमर में खोंसी
हुई बीड़ी सुलगाता हुआ
ट्रैक्टर की तरह खड़खड़ाती हुई
मृत्यु को इसी घाट पर छोड़कर
हम अपने आँसू पोंछते हुए
धीरे-धीरे लौटने लगते हैं
तो चाँडाल अपने स्वांग से
रहस्य उतारता
अपनी मूँछ के पर्दे में
मुस्कुरा रहा होता है ।
5. जो यह निर्गुण गा रहा है
मैदानों से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते
अंतहीन विषाद चलता है पावों से लकीर बनाता हुआ
कोई घरों से दूर ठोस वृक्षों को खटखटाता है आधी रात
भागे हुए रास्ते बार-बार आते हैं पाँव की स्मृतियों में
वासना उस नदी में डूबती नहीं है जो ऊपर से झरती हुई खो जाती है कुछ दूर जाकर
यहाँ जो सबसे कम आकर्षित करता है वह मोक्ष है
जो सबसे कम जरूरी लगता है वह धर्म है
ईश्वर नहीं है यह ज्ञान कम नहीं है इन पहाङों में
तप इतना ही है कि उल्टा चलकर अब वापिस नहीं लौटा जा सकता है
आत्मा की दाढ़ उगी दिखाई नहीं पङती है
धुएं में दूर से जो धुन दिखता है उठता हुआ
वह फकत देह की कातरता है
मैदानों से जंगल की ओर जाने वाले रास्ते
चलकर तय नहीं होते हैं
जो यह निर्गुण गा रहा है, वह गा रहा है ।
संपर्क :
संजय कुमार शांडिल्य
सहायक अध्यापक
सैनिक स्कूल गोपालगंज
पत्रालय-हथुआ
जिला-गोपालगंज (बिहार)
पिन – 841436
मोबाइल - 9431453709
ईमेल – shandilyasanjay1974@gmail.com
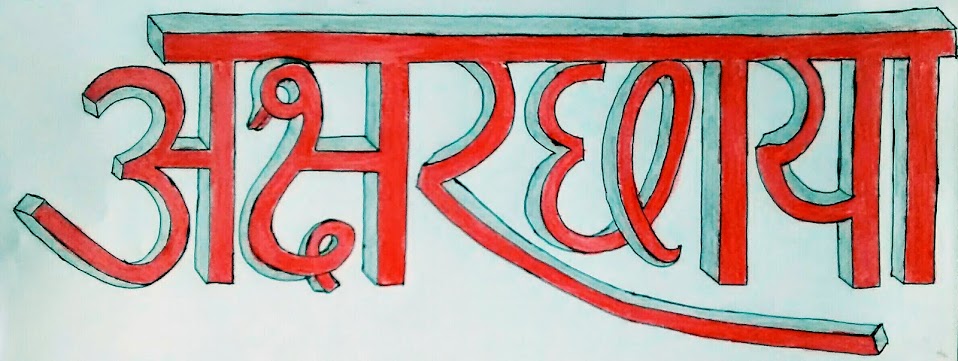


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें